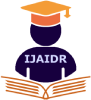
Journal of Advances in Developmental Research
E-ISSN: 0976-4844
•
Impact Factor: 9.71
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 16 Issue 1
2025
Indexing Partners
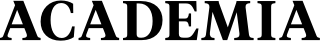













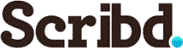




भ्रमरगीत: शहरी विकास की छाया में बदलता ग्रामीण जीवन
| Author(s) | कौशल कुमार शर्मा |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | भक्ति काव्य परंपरा में "भ्रमरगीत" का विशेष स्थान है। यह केवल एक संवादात्मक काव्य नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति का दर्पण भी है। सूरदास के भ्रमरगीत प्रसंग में उद्धव और गोपियों के संवाद के माध्यम से एक गहरी सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। वर्तमान संदर्भ में, यदि इस काव्य को शहरीकरण और ग्रामीण जीवन के द्वंद्व से जोड़ा जाए, तो यह विषय अधिक प्रासंगिक हो जाता है। शहरी विकास ने ग्रामीण जीवन की संरचना, परंपराओं, और सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित किया है। यह शोधपत्र "भ्रमरगीत" के आलोक में ग्रामीण समाज की बदलती स्थितियों और शहरीकरण के प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास करेगा। शहरीकरण केवल भौतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचनाओं को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने ग्रामीण समाज के मूल्यों, परंपराओं और जीवनशैली पर गहरा प्रभाव डाला है। खेतिहर समाज से व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्र में प्रवास, पारंपरिक पेशों का ह्रास, तथा संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन शहरीकरण के प्रत्यक्ष प्रभावों में शामिल हैं। सूरदास का भ्रमरगीत एक ओर जहां ग्रामीण जीवन की सहजता और प्रेम को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर उद्धव जैसे चरित्र के माध्यम से शहरी (या वैचारिक रूप से विकसित) दृष्टिकोण को सामने रखता है। जब गोपियां उद्धव के तर्कपूर्ण योगमार्ग को नकारती हैं और अपने प्रेम व भक्ति मार्ग पर अडिग रहती हैं, तो यह ग्रामीण संस्कृति की दृढ़ता और सहजता का परिचायक बन जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आज भी ग्रामीण जीवन अपनी सादगी और भावनात्मक गहराई के लिए जाना जाता है, जबकि शहरीकरण ने तर्क, आधुनिकता और सुविधाओं की प्राथमिकता को बढ़ावा दिया है। बीज – शब्दः शहरीय सभ्यता, बाज़ारवाद प्रतिवाद साधारणीकरण व्यापारी पूँजीवाद, भक्ति आन्दोलन, ब्राह्मणवाद, जातीय परंपरा, लोकधर्मी, सगुणभक्ति, ग्रामीण संस्कृति, , प्रतिरोध । मूल आलेख भक्ति आंदोलन भारत के लिए द्रविड़ प्रदेश की एक महत्वपूर्ण देन है, जहाँ इसे एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में आकार दिया गया। इस आंदोलन में भक्ति ही मुख्य थी, और इसमें मानवीयता का प्रचुर योगदान था। भक्ति आंदोलन की यह समन्वित दृष्टि ब्राह्मणों के लिए स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि इसमें समभावना की ऊर्जा थी। "भगवद गीता की रचना के लगभग हज़ार वर्षों बाद, जब लोक की यह लहर आलवारों के माध्यम से एक महान धार्मिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुई, तब ब्राह्मण व्यवस्था को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्राह्मणों ने इसे नीच जातियों की दास मानसिकता और अतिभावुकता से जोड़ा था। लेकिन जब आलवार संतों ने इसे पूरे द्रविड़ प्रदेश में एक महान धार्मिक आंदोलन के रूप में स्थापित किया, तब ब्राह्मणों के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा" (भक्ति आंदोलन : इतिहास और संस्कृति, सं. कुँवरपाल सिंह, वाणी प्रकाशन, 2008, पृ. 103)। यह भी संभव है कि ब्राह्मणों द्वारा इसे स्वीकार करने का दूसरा कारण यह था कि इस वैष्णव भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म को शक्ति प्रदान की। जब इस्लाम धर्म एक चुनौती बनकर उभरा, तब हिंदू धर्म में आस्था को प्रोत्साहित करने में भक्ति आंदोलन को सहायक माना गया। "नवीं सदी के आरंभ में शंकराचार्य संस्कृत भाषा में अपने विचारों का प्रचार हिंदू धर्म के उत्थान के लिए कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें आम जनता की पहुँच से बाहर थीं। उसी समय में आलवार और नायनार भक्त अपनी भक्ति के अनुभवों की अभिव्यक्ति के रूप में गीत गाते हुए गाँवों और गलियों में घूमने लगे। सरल तमिल भाषा में रचित भक्तिगीतों का शीघ्र ही सामान्य जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके गीतों में वर्णित विष्णु और शिव की प्रतिष्ठा हिंदू धर्म के प्रति जनता के मन में बढ़ने लगी" (ए. श्रीधर मेनन, केरल का इतिहास, डी.सी. बुक्स, 2021, पृ. 152-153)। यह भी उल्लेखनीय है कि भक्ति आंदोलन को शासकीय संरक्षण भी मिल रहा था। आलवारों में एक कुलशेखर आलवार चेर साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 'पेरूमाल तिरूमोषी' लिखा। इसी तरह, शैवों में चेरमन पेरूमाल नायनार भी एक राजा थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार, भक्ति आंदोलन ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू धर्म को मजबूती दी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी प्रेरित किया। निश्छल प्रेम और समर्पण की भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की जो विचारधारा उन्होंने प्रस्तुत की, वह जातिवाद और भेदभाव की विरोधाभासी चुनौती थी। यह विचार न केवल भक्ति के रूप में एक साधना का मार्ग था, बल्कि समाज के भीतर व्याप्त ऊँच-नीच के भेद को मिटाने का एक सशक्त प्रयास भी था। यह भी स्पष्ट देखा गया है कि भगवद गीता में जिस ज्ञानयोग और कर्मयोग की प्रतिष्ठा की गई थी, वही भक्ति योग आलवारों ने आगे बढ़ाया। आलवारों का 'दिव्य प्रवन्धम' ग्रंथ भक्ति की श्रेष्ठता और ईश्वर के प्रति समर्पण को रेखांकित करता है, और यही तत्व तमिलनाडू के शूद्रकवि नम्मालवार से लेकर हिंदी के कवि सूरदास तक की भक्ति काव्यधारा में देखा जा सकता है। आलवारों और अन्य भक्ति कवियों ने वेदों और शास्त्रों के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए बाह्य ब्राह्मणवाद से परे एक सरल और सुलभ भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। यही भक्ति उस समय के जटिल और दार्शनिक उपदेशों से सामान्य जनता को जोड़ने का प्रयास था, जो कभी दार्शनिक और रहस्यवादी रूप में परिवर्तित हो जाते थे। इस संदर्भ में निर्गुण भक्ति की प्रमुखता पर बल दिया गया, जिसमें ईश्वर को मूर्त रूप से परिभाषित करने के बजाय अमूर्त रूप में पूजा की गई। यह भक्ति का रूप न केवल ईश्वर के निराकार रूप की प्रतिष्ठा करता था, बल्कि जाति और धर्म के भेद को तोड़ने का एक प्रभावी कदम भी था। निर्गुण भक्ति का केन्द्र शहरी क्षेत्रों में था, और डॉ. विनोदशाही के अनुसार, "निर्गुण धारा का महत्व मुख्यतः शहरी विकास से जुड़ी सांस्कृतिक परिवर्तन की चेतना से है। इसका केन्द्र वे नगर थे, जो व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध हो रहे थे और जहां शिल्पकारों तथा बनियों के लिए नए विकास की संभावनाएँ उत्पन्न हो रही थीं।" कबीर और रैदास जैसे संतों ने इस वैकल्पिक पंथ और धर्म को आधार देकर शिल्पकारों और व्यापारियों के बीच भक्ति को बढ़ावा दिया, जबकि गुरु नानक ने व्यापारिक वर्ग को इस दिशा में प्रेरित किया। कबीरदास ने शहरों को केन्द्र बनाकर शिल्पकारों, जुलाहों और चमारों जैसी उपेक्षित जातियों को प्रोत्साहित किया। लेकिन अमूर्त ईश्वर की साधना को कुछ लोग समझने में असमर्थ थे, जिस कारण सगुण भक्ति का प्रचार हुआ। सगुण भक्ति का उद्देश्य भक्ति का समाजीकरण था, जिससे इसे सामान्य जनों के लिए सुगम और उपलब्ध कराया जा सके। सूरदास ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कृष्ण भक्ति को न केवल गाँवों तक पहुँचाया, बल्कि उसे एक आनन्ददायक अनुभव भी बनाया। वह भक्ति के माध्यम से ईश्वर के साथ संवाद की संभावना को सामने लाए, और भक्तों और ईश्वर के बीच आत्मीय संबंध को स्थापित किया। इसके लिए उन्होंने मूर्त रूप में ईश्वर को मानवीय रूप में दर्शाया और उनकी लीलाओं को प्रस्तुत किया। यही वह समय था जब अवतारवाद की महत्ता भी प्रकट हुई, और 'सूरसागर' के 'भ्रमरगीत' में भक्ति के इस सामाजीकरण को देखा जा सकता है। सूरदास ने निर्गुण भक्ति की आलोचना करते हुए गोपिकाओं के माध्यम से इसे समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने का प्रयास किया। यह उल्लेखनीय है कि सूरदास ने नारी को एक अद्वितीय सम्मान दिया और कृष्ण भक्ति के माध्यम से स्त्री समाज को भी प्रेम और आदर का स्थान दिया। उन्होंने गोपिकाओं के मुँह से निर्गुण भक्ति की आलोचना की, जो अपने आप में शहरी सभ्यता की आलोचना बनकर उभरी। इतिहास में काशी और मथुरा जैसे विकसित नगरों के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि इन नगरों में व्यापार और उद्योगों का केन्द्र होने के साथ-साथ वेद, धर्म और शास्त्र का वर्चस्व था। सूरदास ने 'भ्रमरगीत' के माध्यम से इस शहरी सभ्यता और सामंती व्यवस्था के खिलाफ प्रतिवाद व्यक्त किया, और इस प्रकार यह एक उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण की संभावना प्रस्तुत करता है। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद, व्रजवासियों की तप्त प्रेम भावना को शांति देने और उन्हें निर्गुण ब्राह्म, योग और साधना के उपदेश देने के लिए कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को व्रज भेजा। जब उद्धव गोपिकाओं से मिले, तो वे उन्हें एक शहरी व्यापारी के रूप में देखती हैं, जो ज्ञानयोग की उपदेश की बरी-बरी माल लेकर गाँव में आया है। गोपिकाएँ उद्धव को व्यापारी के रूप में देखती हैं, जो ज्ञान और योग के बोझ को गाँव में उतारने का प्रयास कर रहा है। वे उद्धव की उपदेश की भाषा को, जिसे वे प्रलोभन की भाषा मानती हैं, अस्वीकार करती हैं। उनका कहना है कि उद्धव का ज्ञान व्रज में नहीं बिकेगा और न ही वे हमें धोखा दे सकते हैं। गोपिकाएँ यह महसूस करती हैं कि शहर की सस्ती चीजों को महंगे दाम पर बेचने वाले व्यापारी के शब्दों से वे ठगी नहीं खा सकतीं। वे इस प्रकार के प्रलोभनों में नहीं फँसना चाहतीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह व्यापारियों का धंधा है, जो स्वयं को गुलाम बनाने का काम करते हैं। यह दृश्य गाँव और शहर, तथा बाज़ार और ग्रामीण जीवन के बीच के भेद को उजागर करता है। कबीरदास ने भी अपने समय में बाज़ार के विस्तार को पहचानते हुए इच्छाओं पर नियंत्रण की बात की थी, और इस पर काबू पाने का आह्वान किया था। आगे चलकर, औपनिवेशिक काल में भारतेन्दु ने भी 'अन्धेर नगरी' के माध्यम से लोभ और भ्रामक बाज़ार व्यवस्था से दूर रहने का संकेत दिया था। गोपिकाएँ इस उपदेश को शहरी सभ्यता के प्रलोभन के रूप में देखती हैं, जिसे वे ठगने का प्रयास मानती हैं। उनके अनुसार, उद्धव की भाषा केवल मुक्ति की लुभावनी बातों को सामने लाकर उन्हें धोखा देने के लिए है। गोपिकाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि वे उस झाँसे में नहीं आएंगी, क्योंकि वे लोभी नहीं हैं, जैसा कि शहरी लोग होते हैं। सूरदास की गोपिकाएँ मुक्ति के मोह में प्रेम को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होतीं। उनके लिए ज्ञान और योग की बातें समझ से बाहर हैं, और वे केवल प्रेम को ही स्वीकार करती हैं। एक स्थान पर वे कहती हैं, "मोहिं अलि दुहूँ भांति फल होत, तब रस-अधर लेति मुरली, अब भई कूवरी सोत..." अर्थात, "तुम्हारे योग में संसार से उदासीन रहने की बात है, लेकिन हम पहले ही कृष्ण के ध्यान में लीन हैं और इसलिए संसार से उदासीन हैं। तुम्हारी बातें मथुरा में समझने वाले लोग हैं, लेकिन इस व्रज में हम केवल कृष्ण के रूप में ही जीवन का रस पा रहे हैं।" इसके बाद वे यह भी कहती हैं, "फिरि फिरि कहा सिखावत मौन, दुसह वचन अलि यों लागत उर ज्यों जारे पर लौन सूर आज लौं सुनी न देखी जोत सूतरी पोहत..." अर्थात, "तुम हमें जो उपदेश दे रहे हो, वह हम पर नहीं चलता। हमारे लिए घर और वन एक जैसे हैं, और हम तुम्हारे कहने से किसी और रास्ते पर नहीं चल सकतीं। हम तुम्हें एक सलाह देती हैं कि तुम अपना योग का उपदेश उन लोगों को दो जिन्हें संसार के भोगों और ऐश्वर्य में आसक्ति है।" गोपिकाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि वे शहर की भोगवादी जीवनशैली से परे हैं और अपने प्रेम को केवल कृष्ण के लिए ही समर्पित करती हैं। वे कहती हैं, "हम कृष्ण के सिवा किसी और से प्रेम कैसे कर सकते हैं? हमने अपना हृदय पहले ही कृष्ण को समर्पित कर दिया है, और अब हम दूसरों से प्रेम कैसे कर सकती हैं?" उनकी यह भावना वर्तमान समाज की उपभोक्तावादी और 'यूज़ एंड थ्रो' संस्कृति की आलोचना के रूप में देखी जा सकती है। गोपिकाएँ प्रेम को एक अदृश्य, निष्कलंक और निःस्वार्थ भावना के रूप में देखती हैं। उनका प्रेम केवल भोग या तृप्ति के लिए नहीं है, बल्कि उसमें सतीत्व और स्थिरता की गहरी भावना है। वे कहती हैं, "क्या यह कोई भजन हो सकता है, जिसमें प्रिय के अतिरिक्त किसी और से प्रेम किया जाए?" गोपिकाएँ यह सिद्ध करती हैं कि वे केवल कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं, और इसी प्रेम के लिए वे सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ने तक तैयार हैं। वे अपने मान-सम्मान की परवाह नहीं करतीं और लोक-लाज को ताक पर रखकर भी अपने पवित्र प्रेम के रास्ते पर चलने में संकोच नहीं करतीं। यहाँ पर स्पष्ट है कि गोपिकाएँ एक निष्कलंक प्रेम की मिसाल प्रस्तुत करती हैं, जो किसी भी भौतिक लाभ या स्वार्थ से परे है। उनके लिए प्रेम किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं, बल्कि एक पूर्ण और शुद्ध भावनात्मक संबंध है, जो समाज की भोगवादी और उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों से दूर है। गोपिकाएँ बेलों से रूपक बाँधते हुए उद्दव से कहती हैं, "मधुकर, हम वे लताएँ नहीं हैं जिनसे तुम रस लेकर फिर कहीं और उड़ जाते हो। तुम्हारी तरह हम किसी बेल से रस निकालकर उसे छोड़ने वाली नहीं हैं। तुम्हारा यह स्वभाव भौंरे जैसा है, जो एक फूल से रस लेकर दूसरे पर उड़ जाता है, बिना किसी बेल या फूल से लगाव के। हम ऐसे प्रेम के योग्य नहीं हो सकतीं।" यहाँ पर गोपिकाएँ कृष्ण की आलोचना करती हैं कि वे अपने आत्मसम्मान को नष्ट नहीं करना चाहतीं, और इस तरह वे प्रेम को किसी व्यक्ति से परे, केवल भौतिक उपभोग तक सीमित नहीं करना चाहतीं। वे कृष्ण के बारे में व्यंग्य करती हैं कि भले ही उनका प्रेम असाधारण था, फिर भी कृष्ण ने उन्हें धोखा दिया और मथुरा में बसने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने कंस की दासी को प्रेम की अंधकारिणी बना दिया। वे कहती हैं कि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम सच्चा था, फिर भी कृष्ण ने उन्हें त्याग दिया और किसी और को अपना लिया। यह स्थिति श्रद्धा और इडा की तरह है, जहाँ श्रद्धा मनु को संजीवित करने में विफल रही, और इडा ने अंततः अपना हृदय पाया। यहाँ गोपिकाएँ इस हार और तिरस्कार की गहरी व्यथा को व्यक्त करती हैं, हालांकि वे श्रद्धा के समान शहर के आकर्षण से दूर हैं। गोपिकाएँ कहती हैं कि शहर केवल कामनाओं और भोगों का स्थान है, जहाँ केवल मनोरंजन और क्षणिक सुख की खोज होती है। वे उद्धव और कृष्ण को व्यंग्य के रूप में "भौंरे" कहती हैं, जो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के प्रभाव से प्रभावित होकर पुरानी यादों को भूल जाते हैं। गोपिकाएँ इस शहरीकरण को भौतिकता और भोगवाद के प्रतीक के रूप में देखती हैं, जहाँ व्रज के गांवों के नैतिक मूल्य, संस्कार और सामाजिक संबंध मिट रहे हैं। उनके अनुसार, मथुरा के लोग छल, कपट और चालाकी में विश्वास करते हैं, और वे उद्धव से कहती हैं कि मथुरा में कोई भी धर्मात्मा नहीं है। वहाँ पर केवल लोग स्वार्थी और कपटी हैं, जो सिर्फ अपने हित में जीते हैं। गोपिकाएँ मथुरा और शहरों की आलोचना करती हैं, यह कहते हुए कि नगरों की सभ्यता ने गाँवों को नष्ट किया है। वे यह भी बताती हैं कि इस भौतिकता और नफ़रत की संस्कृति ने ही साम्राज्यवादियों के लिए रास्ता खोला था। गोपिकाएँ कृष्ण को भी इस स्थिति में देखती हैं, जहां वह उस गांव, प्रकृति और लोक से विमुख हो गए हैं, जिन्होंने उन्हें अपनी मुरली से अभिभूत किया था। यहाँ तक कि कृष्ण भी अब साम्राज्यवादी आकर्षण की ओर मुड़ गए हैं, जैसा कि मथुरा में रहने के बाद स्पष्ट होता है। गोपिकाएँ यह मजाक करती हैं कि मथुरा में दो हंस हैं—एक अक्रूर और दूसरा उद्दव। ये दोनों अपनी चालाकियों और कुटिलताओं को अच्छे से जानते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वे कंस को हराकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। गोपिकाओं के शब्दों में, मथुरा और शहरों में उनके प्रेम की कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ अब न तो कोई ईमानदारी है, न ही आत्मीयता, और न ही किसी प्रकार का विश्वास। यह सब उस पश्चिमी सभ्यता की उपज है, जिसने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। गोपिकाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि वे प्रेम में निष्कलंक और निःस्वार्थ हैं, और उनके लिए गाँव के नैतिक मूल्य और उनके आत्मगौरव से बढ़कर कुछ नहीं है। गोपिकाएँ शहर के ज्ञानयोग या बुद्धिवाद को अस्वीकार करती हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। उनके लिए प्रेम ही सर्वोत्तम है, और वे इसे अपनी साधना मानती हैं। उनके लिए विरह ही एकमात्र साधना है, और इसके अलावा किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं है। वे कहती हैं, "ऊधो, व्रज में पैंठ करी, यह निर्गुण निर्मूल गाठरीं, अब किन करहू खरी। हम ग्वालिन, गोरस दधि बेंचौ, लेहिं अवै सवरी सूर, यहाँ कोऊ ग्राहक नाहीं, देखियत गरे परी।" (वहीं, पृ. 220-221) यहाँ गोपिकाएँ उद्धव से यह कहती हैं कि वे निर्गुण ब्राह्मण के ज्ञान और उसकी वस्तुओं को बेचने की कोशिश न करें, क्योंकि गाँव के लोग उन वस्तुओं को खरीदने के योग्य नहीं हैं। वे यह स्पष्ट करती हैं कि उनका कोई दिलचस्पी उस प्रकार के ज्ञान या वस्तु में नहीं है। वे कृष्ण से कहती हैं कि यदि वह गोरस और दही बेचने के लिए तैयार हों, तो वे उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करेंगी, क्योंकि यही उनके लिए प्रिय है। यहाँ पर केवल गोपिकाएँ ही नहीं, बल्कि गायें भी कृष्ण के विरह में तड़प रही हैं। वे उन्हीं स्थानों को ढूँढती फिरती हैं, जहाँ कृष्ण ने गायों का दूध दुहा था। और जब वे वहाँ पहुंचती हैं, तो पछाड़ खाकर गिर पड़ती हैं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। गोपिकाएँ उद्दव के सामने गाँव के मूल्यों की प्रतिष्ठा करती हैं। वे निष्ठा, निस्वार्थता, आत्मीयता और ईमानदारी के महत्व को व्यक्त करती हैं, और अंततः शहर के ज्ञानयोग और बुद्धिवाद का प्रतिरोध करती हैं। उनके लिए प्रेम का अर्थ केवल कृष्ण से नहीं, बल्कि पूरी व्रज भूमि, वहाँ की प्रकृति और वहाँ के समाज से जुड़ा है। यहाँ प्रेम और सह-अस्तित्व की भावना है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। सूरदास यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर प्रेम का सही अर्थ मनुष्य और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, सहयोग और समर्पण की भावना है। यह भक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाजिक और प्राकृतिक सहयोग का भी प्रतीक है। व्रज की भक्ति में हर व्यक्ति, हर प्राणी और प्रकृति के साथ एक संबंध है, जो प्रेम और सहयोग की भावना पर आधारित है। व्रज की याद कभी भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि मथुरा, एक वैभवशाली नगरी होते हुए भी, व्रज की याद के सामने कुछ भी नहीं। सूरदास यही सिद्ध करना चाहते हैं कि मथुरा का भव्यता और शहरी दुनिया के तत्व व्रज के शुद्ध, सरल प्रेम के सामने मूल्यहीन हो जाते हैं। इसे केवल नोस्टाल्जिया के रूप में न देखकर, इसे गाँव की जीवंत परंपरा, लोक संस्कृति और उसमें समाहित मूल्यों को पुनः स्थापित करने की आकांक्षा के रूप में देखा जा सकता है। जबकि आजकल इन मूल्यों से निर्वासन की प्रक्रिया लगातार जारी है। सूरदास ‘भ्रमरगीत’ में निर्गुण के मुकाबले सगुण की विजय दिखाना चाहते हैं, जो अंततः शहर की संकुचित बुद्धिवाद के खिलाफ गाँव के आदर्शों की जीत होती है। वे गोपिकाओं के सरल और निश्छल प्रेम के समक्ष उद्धव की हार को दर्शाकर ज्ञानयोग की पराजय और वृद्धिवाद की असफलता को उजागर करते हैं। यह वही प्रयास है जो जयशंकर प्रसाद ने ‘कामायनी’ में किया है। ‘भ्रमर गीत’ में शहर और गाँव के बीच के द्वंद्व को बारीकी से चित्रित किया गया है। इसे केवल गोपिकाओं के उलाहने और वाक् वैचित्र्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसमें एक गहरे सांस्कृतिक विमर्श का तत्व समाहित है, जिसमें शहरी अवांछित मूल्यों के प्रसार को और उन पर प्रतिरोध करने की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। भारतीय परंपरा में जीवन का परम श्रेय दुःखों के आत्यन्तिक विनाश और आनंद की प्राप्ति को माना गया है। आत्मपूर्णता भी एक अन्य अपेक्षा से जीवन का परम श्रेय मानी जाती है। तात्त्विक दृष्टि से परम श्रेय हमारी सत्ता का सारतत्त्व है, जिसे जैन परंपरा में स्वभावदशा की उपलब्धि और गीता में परमात्मा की प्राप्ति कहा गया है। संक्षेप में, इसे निर्वाण कहा जाता है, और विस्तार से विचार करें तो यह हमारी सत्ता का सार, आनंद की अवस्था और दुःखों से मुक्ति है। भारतीय परंपरा में मोक्ष, परम श्रेय, निर्वाण, परमात्मदशा, स्वभावदशा आदि पर्यायवाची शब्द हैं। वस्तुतः भारतीय दृष्टिकोण से शुभ और परम शुभ में अंतर है। परम शुभ आध्यात्मिक आदर्श है, जबकि शुभ लौकिक आदर्श है, जिसे पुण्य भी कहा जाता है। पुण्य का परोपकार एक ऐसा आदर्श है जिसका उद्देश्य दूसरों का भला करना है, जिसे हम सामाजिक जीवन का आदर्श भी कह सकते हैं। शुभ के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला आचरण “उचित” और अशुभ की ओर उन्मुख आचरण “अनुचित” कहलाता है। उचित का अर्थ समाजिक नियमानुसार होता है, और शुभ का संबंध साधन और साध्य से है। कोई कार्य यदि नैतिक नियमों के अनुरूप किया गया हो, तो वह उचित होता है, जबकि नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया कार्य अनुचित होता है। सामाजिक और नैतिक संदर्भ में सद्गुण मनुष्य की वह श्रेष्ठ स्थायी मनोवृत्ति है, जिसका निरंतर विकास करना पड़ता है और जो हमेशा आचरण में अभिव्यक्त होती है। सद्गुण व्यक्ति के स्वभाव का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं, जो उसे अपने नैतिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये जन्मजात प्रवृत्तियों जैसे भूख, प्यास, कामवासना, भय, क्रोध और प्रेम से भिन्न होते हैं, क्योंकि इनका विकास निरंतर अभ्यास और प्रयास से होता है। सद्गुणों का महत्व व्यक्ति और समाज दोनों के लिए है। गीता में व्यक्ति और समाज के लिए अलग-अलग सद्गुणों का भेद नहीं किया गया है, क्योंकि दोनों एक-दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। हालांकि, गीता के तीसरे अध्याय के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की मानसिकता और समाज के आधार पर ज्ञानी और कर्मयोगी में भेद किया जा सकता है, और इसी आधार पर नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों में विभाजन संभव है। नैतिक और सामाजिक सद्गुणों में संयम, मैत्री, उदारता, संतोष, दृढ़ता, अहिंसा, क्षमा, शुद्धता, अभय, सत्य आदि को शामिल किया जा सकता है, जबकि बौद्धिक सद्गुणों में ज्ञान और स्वाध्याय की महत्ता है। हालांकि, इन दोनों के बीच भेद करना पूरी तरह उचित नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बिना सभी सद्गुण अपना वास्तविक अर्थ और प्रभाव खो देते हैं। इस प्रकार, हमारे व्यावहारिक निर्णयों को प्रभावित करने वाले मूल्य एकत्रित होते हैं, और यही दृष्टिकोण अतीन्द्रिय विषयों के अनुचिन्तन और अनुसंधान में भी लागू होता है, जहां बौद्धिक साधना का उद्देश्य किसी विषय को प्राप्त करना या उससे मुक्ति पाना होता है। मूल्य ज्ञान में विषय ज्ञान और आत्मज्ञान का सम्मिलन होता है, और आत्मज्ञान में एक अविषयात्मक अपरोक्षता पाई जाती है, जो मूल्यज्ञान को अधिक समृद्ध और सूक्ष्म बना देती है। इस प्रकार, मूल्य अनुभूति के माध्यम से दुनिया को अर्थ देने वाले तत्व होते हैं, हालांकि ये दुनिया की कालिक सत्ता का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि ये तटस्थ होते हैं, जबकि मूल्य स्वयं अनुभव के सारांश होते हैं। सिजविक के शब्दों में, "हम व्यक्ति को केवल समाज के सदस्य के रूप में जानते हैं। जो गुण हम कहते हैं, वे मुख्यतः समाज के सदस्यों के साथ उनके व्यवहार में प्रकट होते हैं, और उनकी सबसे बड़ी खुशियाँ उनके सहवास से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार यह धारणा कि मानव का सर्वोच्च शुभ उसके सामाजिक संबंधों से स्वतंत्र है, एक विरोधाभास है। इसलिए व्यक्ति का परम शुभ समाज के परम शुभ पर आधारित है, क्योंकि वह समाज का अभिन्न अंग है। नीतिशास्त्र का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक हित, स्वार्थ और परार्थ में सामंजस्य स्थापित करना है।" मूल्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन यह सिद्ध करता है कि सभी मूल्य एक-दूसरे से परिमाण में जुड़े होते हैं, और प्रत्येक शुभ या मूल्य को तोलकर उसका स्थान एक निरंतर विकसित होती उच्चतम से निम्नतम मूल्य श्रेणी में निर्धारित किया जा सकता है। विभिन्न शुभों का मूल्यांकन करते समय उनकी राशि और गुण दोनों का ध्यान रखना आवश्यक है। मूल्य के गुणात्मक भेद यह स्पष्ट करते हैं कि जब हमें निम्न और उच्च मूल्य के बीच चयन करना हो, तो हमें सदैव उच्च मूल्य का चयन करना चाहिए। इसीलिए, कोई भी शुभ चाहे मात्रा में अधिक हो, वह दूसरे प्रकार के शुभ की पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए, जब परिस्थितियाँ हमें सभी प्रकार के शुभों को प्राप्त करने का अवसर नहीं देतीं, तब हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि उनमें से कौन सा सबसे श्रेष्ठ शुभ है, जिसे प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक और नैतिक ज्ञान यह बताता है कि वही कर्म उचित है जो शुभ का सृजन करता है। जब विभिन्न शुभों में से किसी एक का चयन करना हो, तो उस शुभ का चयन करना चाहिए, जो अधिकतम शुभों को उत्पन्न करता है। आज के समय में, सभी मूल्य, सद्गुण और आदर्श हमारे सामने चुनौती के रूप में होते हैं, जिन पर निरंतर चिंतन और मंथन आवश्यक है ताकि हम इन्हें और अधिक परिष्कृत कर सकें और समाज में उनके प्रभाव को सशक्त बना सकें। सन्दर्भ सूची- 1. मल्लिक, सुनील, सामाजिक एवं नैतिक दृष्टिकोण, कोलकाता: यूनिवर्सल प्रकाशन, 2017 2. बेन, विक्रम, आध्यात्मिकता और मूल्य: भारतीय दृष्टिकोण, दिल्ली: आचार्य प्रकाशन, 2018। 3. मौर्य, सुधीर, नैतिकता और समाज में उसका स्थान, जयपुर: धर्म प्रकाशन, 2016। 4. श्रीवास्तव, देवेंद्र, मूल्य और समाज की संरचना, लखनऊ: काशी वर्धन, 2017। 5. झा, रवि, नैतिकता और आदर्श: एक दृष्टिकोण, पटना: प्रकाशक का नाम, 2019। 6. कुमार, सुरेश, समाजशास्त्र और भारतीय परंपराएँ, मुंबई: आदर्श प्रकाशन, 2014। 1. तिवारी रामचंद्र करंट आईएफ यू इन सोशल साइंस साइंसेज कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स दिल्ली 2008 2. डॉ मंजू लता भारती सामाजिक समस्याएं अर्जुन पब्लिशिंग हाउस दिल्ली 2012 3. यादव डॉक्टर सागर सिंह त्यागी डॉक्टर रुचि समाज प्रबंधन और नैतिकता को ऑपरेशन पब्लिकेशन जयपुर 2017 4. ज्ञानोदय मासिक पत्रिका भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी 2010 5. मई दुनिया मासिक पत्रिका 2019 6. www.socialvalues. 7. www.modrdnization |
| Keywords | शहरीय सभ्यता, बाज़ारवाद प्रतिवाद साधारणीकरण व्यापारी पूँजीवाद, भक्ति आन्दोलन, ब्राह्मणवाद, जातीय परंपरा, लोकधर्मी, सगुणभक्ति, ग्रामीण संस्कृति, , प्रतिरोध । |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 16, Issue 1, January-June 2025 |
| Published On | 2025-02-20 |
| Cite This | भ्रमरगीत: शहरी विकास की छाया में बदलता ग्रामीण जीवन - कौशल कुमार शर्मा - IJAIDR Volume 16, Issue 1, January-June 2025. |
Share this

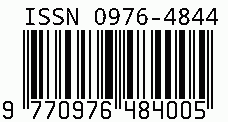
CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJAIDR DOI prefix is
10.71097/IJAIDR
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

