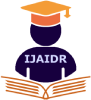
Journal of Advances in Developmental Research
E-ISSN: 0976-4844
•
Impact Factor: 9.71
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 16 Issue 1
2025
Indexing Partners
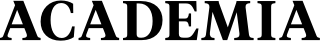




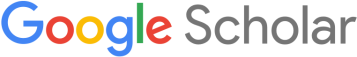








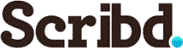




बौद्ध शिक्षा केंद्रों की ऐतिहासिक भूमिका एवं वर्तमान शिक्षा पर उनका प्रभाव
| Author(s) | राजेंद्र मीणा, डॉ चंद्रशेखर शर्मा |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | बौद्ध शिक्षा प्रणाली प्राचीन भारत में ज्ञान और बौद्धिक परंपराओं के विकास का एक प्रमुख आधार रही है। विशेष रूप से नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, और ओदंतपुरी जैसे बौद्ध शिक्षा केंद्रों ने भारतीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक बौद्धिक और शैक्षिक परंपराओं को प्रभावित किया। इन शिक्षा केंद्रों में न केवल धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था, बल्कि दर्शन, चिकित्सा, खगोलशास्त्र, व्याकरण, और तर्कशास्त्र जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। इन शिक्षा संस्थानों में विद्वानों और छात्रों के बीच गहन संवाद, बहस, और बौद्धिक विमर्श की परंपरा विकसित हुई, जिसने ज्ञान के विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध शिक्षा केंद्रों की एक विशेषता यह थी कि वे मात्र बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य समुदायों के लिए भी खुले थे। विभिन्न देशों के छात्र यहाँ अध्ययन करने आते थे, जिससे ये केंद्र बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय बौद्धिक संवाद के केंद्र बन गए। उदाहरणस्वरूप, नालंदा विश्वविद्यालय में चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति, सैन्य विज्ञान, चिकित्सा और काव्यशास्त्र जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध शिक्षा केवल आध्यात्मिक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका व्यापक सामाजिक और व्यावसायिक प्रभाव भी था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी इसका शिक्षक-छात्र संबंध। शिक्षा की प्रक्रिया केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि छात्रों को जीवन कौशल, नैतिकता, और मानसिक अनुशासन में भी प्रशिक्षित किया जाता था। शिक्षकों और छात्रों के बीच एक गहरा बौद्धिक रिश्ता था, जिसमें संवाद और तर्क-वितर्क को प्रोत्साहित किया जाता था। इस प्रणाली में गुरु और शिष्य के बीच सम्मानजनक संबंध की अवधारणा विकसित हुई, जो आज भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के नैतिक मूल्यों में देखी जा सकती है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि यह ज्ञान को दान (दानपरमिता) और लोककल्याण का साधन मानती थी। इसके अंतर्गत विद्या को केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम न मानकर समाज के कल्याण के लिए उपयोगी बनाने पर जोर दिया जाता था। इस दृष्टिकोण ने शिक्षा को एक नैतिक और समाजोपयोगी गतिविधि के रूप में स्थापित किया, जो वर्तमान समय में शिक्षा के उद्देश्य के रूप में पुनः प्रासंगिक होता जा रहा है। आज के संदर्भ में जब शिक्षा प्रणाली नैतिकता, मानवता, और समावेशिता के प्रश्नों से जूझ रही है, बौद्ध शिक्षा केंद्रों के मूल्यों का पुनः मूल्यांकन आवश्यक हो गया है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यावसायिकता के बढ़ते प्रभाव के बीच बौद्ध शिक्षा का नैतिक और समावेशी दृष्टिकोण प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। वर्तमान में उच्च शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, और ध्यान (माइंडफुलनेस) जैसी अवधारणाएँ पुनः लोकप्रिय हो रही हैं, जो बौद्ध शिक्षाशास्त्र से प्रेरित हैं। यह अध्ययन प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्रों की ऐतिहासिक भूमिका का विश्लेषण करेगा और आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर उनके प्रभाव को समझने का प्रयास करेगा। इसके माध्यम से हम यह जान सकेंगे कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली की कौन-सी विशेषताएँ आज भी प्रासंगिक हैं और उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार समाहित किया जा सकता है। बौद्ध शिक्षा केंद्रों की ऐतिहासिक भूमिका प्राचीन भारत के बौद्ध शिक्षा केंद्र न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के बल्कि वैश्विक शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे, जहाँ विभिन्न देशों के छात्र अध्ययन के लिए आते थे। इन संस्थानों ने शिक्षा को संरचित रूप में विकसित किया और भारत को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बनाया। बौद्ध शिक्षा केंद्रों की प्रणाली अत्यंत उन्नत थी और यह केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी, बल्कि विभिन्न शास्त्रों, विज्ञानों और कलाओं का समावेश करती थी। इन संस्थानों में शिक्षा मौखिक परंपरा के साथ-साथ लिखित रूप में दी जाती थी, और शिक्षण पद्धति में संवाद, विमर्श और ध्यान (मेडिटेशन) को प्रमुखता दी जाती थी। इस प्रकार, इन शिक्षा केंद्रों ने न केवल बौद्ध विचारधारा के प्रचार-प्रसार में योगदान दिया, बल्कि ज्ञान-विज्ञान और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से वैश्विक शिक्षा को भी समृद्ध किया। 1. नालंदा विश्वविद्यालय (5वीं - 12वीं शताब्दी) नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध और सुव्यवस्थित शिक्षा केंद्र था। इसे विश्व का प्रथम पूर्ण विश्वविद्यालय माना जाता है, जिसकी स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम (लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी) ने की थी। यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जहाँ बौद्ध दर्शन के साथ-साथ अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, जैसे कि व्याकरण, आयुर्वेद, गणित, तर्कशास्त्र, खगोलशास्त्र, योग, और वैदिक अध्ययन। नालंदा में शिक्षकों और छात्रों का एक विशाल समुदाय था, जिसमें चीन, तिब्बत, कोरिया और दक्षिण-पूर्व एशिया से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। नालंदा में शिक्षा प्रणाली अत्यंत उन्नत थी, और यहाँ के पुस्तकालय (धर्मगंज) में हजारों पांडुलिपियाँ संरक्षित थीं। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ अध्ययन किया और अपने यात्रा वृत्तांत में उल्लेख किया कि नालंदा में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। यहाँ अध्ययनरत छात्र केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं रहते थे, बल्कि तार्किक तर्क-वितर्क और गहन बौद्धिक चर्चाओं में भाग लेते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का योगदान बौद्ध महायान परंपरा के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण था, और इसका प्रभाव भारत के अलावा तिब्बत, चीन, जापान और अन्य एशियाई देशों में भी देखा जा सकता है। 2. तक्षशिला विश्वविद्यालय (6वीं सदी ईसा पूर्व - 5वीं सदी ईस्वी) तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन विश्व का एक अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित था। यह विश्वविद्यालय 6वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी ईस्वी तक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। इसे औपचारिक रूप से "विश्वविद्यालय" नहीं कहा जाता था, क्योंकि इसमें एक केंद्रीय संस्था नहीं थी, बल्कि अनेक स्वतंत्र शिक्षकों के समूह अलग-अलग विषयों का शिक्षण कराते थे। यहाँ अध्ययन करने वाले प्रमुख विद्वानों में चाणक्य (कौटिल्य), महान वैयाकरण पाणिनि, और आयुर्वेदाचार्य चरक शामिल थे। तक्षशिला में विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाए जाते थे, जिनमें चिकित्सा, सैन्य विज्ञान, राजनीति, खगोलशास्त्र, गणित, भाषा विज्ञान, और दर्शनशास्त्र प्रमुख थे। यहाँ की शिक्षा पद्धति व्यावहारिक और तार्किक दृष्टिकोण पर आधारित थी, जो विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की गहन समझ प्रदान करती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह एक बहु-सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र था, जहाँ भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ग्रीक, फारसी, और मध्य एशियाई छात्र भी शिक्षा ग्रहण करते थे। यह शिक्षा केंद्र सिकंदर महान के आक्रमण के दौरान भी चर्चा में रहा और बाद में इसे कुषाण और गुप्त सम्राटों का संरक्षण प्राप्त हुआ। 3. विक्रमशिला विश्वविद्यालय (8वीं - 12वीं शताब्दी) विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंश के राजा धर्मपाल (8वीं शताब्दी) द्वारा किया गया था। यह बिहार में स्थित था और विशेष रूप से बौद्ध महायान अध्ययन और तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध था। विक्रमशिला को नालंदा के समकक्ष माना जाता था और इसे तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में सहायक माना जाता है। इस विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती थी, और यहाँ की प्रवेश परीक्षा कठिन होती थी। यहाँ विद्यार्थियों को ध्यान, तंत्र, दर्शन, व्याकरण, और अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। विक्रमशिला की शिक्षा प्रणाली अत्यंत व्यवस्थित थी और यहाँ नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के साथ संवाद होते थे। यह विश्वविद्यालय तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु अतीश दीपंकर का प्रमुख अध्ययन केंद्र भी था, जिन्होंने बाद में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 4. वल्लभी और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था और इसे प्रशासनिक एवं विधि अध्ययन के लिए जाना जाता था। यह विश्वविद्यालय पश्चिमी भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, जहाँ बौद्ध ग्रंथों के साथ-साथ न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई भी की जाती थी। वल्लभी विश्वविद्यालय व्यापार और प्रशासन के क्षेत्र में अपने विशेष पाठ्यक्रमों के कारण प्रसिद्ध था और यहाँ से अध्ययन करके निकलने वाले छात्र विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होते थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र था, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासकों द्वारा की गई थी। यह बौद्ध धर्म के अध्ययन और शोध का प्रमुख केंद्र था और यहाँ कई तिब्बती बौद्ध भिक्षु अध्ययन के लिए आते थे। माना जाता है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का विनाश मुहम्मद बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान हुआ, उसी समय जब नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को भी नष्ट कर दिया गया था। बौद्ध शिक्षा केंद्रों ने प्राचीन भारत में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये संस्थान केवल धार्मिक शिक्षण केंद्र नहीं थे, बल्कि इनका प्रभाव विज्ञान, चिकित्सा, प्रशासन, और दर्शन जैसे विषयों में भी व्यापक रूप से देखा जाता है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, और ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालयों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक वैश्विक पहचान दिलाई और एशिया, मध्य एशिया, और अन्य देशों में भारतीय ज्ञान प्रणाली का प्रचार-प्रसार किया। हालांकि मध्यकाल में आक्रमणों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, लेकिन इनका प्रभाव आज भी शिक्षा प्रणाली में देखा जा सकता है। आधुनिक विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, बहस, और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने वाली प्रणालियाँ इन्हीं बौद्ध शिक्षा केंद्रों की शिक्षण पद्धति से प्रेरित हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा, ध्यान (माइंडफुलनेस), और ज्ञान के मुक्त आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जो बौद्ध शिक्षा केंद्रों की विरासत से सीखा जा सकता है। इसलिए, प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्रों की शिक्षाओं और पद्धतियों को पुनः अपनाकर आधुनिक शिक्षा को अधिक नैतिक, समावेशी, और ज्ञानपरक बनाया जा सकता है। बौद्ध शिक्षा केंद्रों के पतन के कारण बौद्ध शिक्षा केंद्रों की स्थापना और उनका विकास भारत को प्राचीन काल में एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने में सहायक रहा, लेकिन मध्यकाल तक आते-आते इनकी स्थिति धीरे-धीरे कमजोर होती चली गई। इसके पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारण थे, जिनके चलते ये शिक्षा केंद्र विलुप्त हो गए। 1. ब्राह्मणवादी शिक्षा प्रणाली का पुनरुत्थान गुप्तकाल के पश्चात हिंदू धर्म में पुनर्जागरण हुआ, जिसके चलते गुरुकुल प्रणाली को अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी। वेदों, उपनिषदों और स्मृतियों पर आधारित ब्राह्मणवादी शिक्षा प्रणाली का विस्तार होने लगा, जिससे बौद्ध शिक्षा केंद्र धीरे-धीरे उपेक्षित होते गए। राजा और अभिजात्य वर्ग ने हिंदू गुरुकुलों को संरक्षण देना शुरू किया, जिससे बौद्ध शिक्षा संस्थानों की महत्ता कम होने लगी। 2. धार्मिक असहिष्णुता और सामाजिक परिवर्तन प्राचीन काल में भारत धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र था, जहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों का सह-अस्तित्व था। लेकिन मध्यकाल में धर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी और बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता बढ़ने लगी। समाज में वैदिक परंपराओं की पुनः प्रतिष्ठा होने से बौद्ध धर्म को धीरे-धीरे हाशिए पर धकेल दिया गया। इसके कारण बौद्ध शिक्षण संस्थानों में छात्रों की संख्या घटने लगी और वे प्रभावहीन हो गए। 3. राजकीय संरक्षण का अभाव बौद्ध शिक्षा केंद्रों को प्रारंभ में शासकों और व्यापारिक समुदायों का भरपूर संरक्षण प्राप्त था। मौर्य, गुप्त और पाल राजाओं ने इन विश्वविद्यालयों को भूमि दान, आर्थिक सहायता और संरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान की थीं। लेकिन जब शासक वर्ग बौद्ध धर्म से विमुख हुआ और अन्य परंपराओं को अपनाने लगा, तब इन संस्थानों को मिलने वाला आर्थिक समर्थन समाप्त हो गया। इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों का पलायन हुआ और धीरे-धीरे ये शिक्षा केंद्र नष्ट हो गए। 4. बौद्ध धर्म की लोकप्रियता में गिरावट 7वीं शताब्दी के बाद से ही भारत में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता में गिरावट आने लगी। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या घटने से उसके संस्थानों को सामाजिक और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। महायान और वज्रयान शाखाओं में विभाजन तथा तांत्रिक प्रभाव के कारण भी इसकी लोकप्रियता घटी। फलस्वरूप, बौद्ध शिक्षा संस्थानों की प्रासंगिकता समाप्त होने लगी। 5. विदेशी शिक्षा केंद्रों का आकर्षण मध्यकाल में भारतीय विद्यार्थियों और विद्वानों ने बौद्ध अध्ययन के लिए तिब्बत, चीन और श्रीलंका जैसे देशों की ओर रुख किया। बौद्ध शिक्षा के नए केंद्र इन देशों में विकसित हुए, जिससे भारत के परंपरागत शिक्षा संस्थान धीरे-धीरे महत्वहीन होते चले गए। इन सभी कारणों के परिणामस्वरूप, बौद्ध शिक्षा केंद्रों का ऐतिहासिक पतन हुआ, और भारत का शिक्षा जगत एक नई दिशा में आगे बढ़ा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर बौद्ध शिक्षा केंद्रों का प्रभाव बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने न केवल प्राचीन भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इसका प्रभाव आज भी वैश्विक शिक्षा प्रणाली में देखा जा सकता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान, नैतिक शिक्षा, समावेशिता और बहु-विषयक अध्ययन जैसी अवधारणाएँ बौद्ध शिक्षा केंद्रों से प्रेरित प्रतीत होती हैं। 1. वैश्विक शिक्षा केंद्रों की अवधारणा नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे बौद्ध शिक्षा केंद्रों ने बहु-विषयक अध्ययन और अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए खुले शिक्षण संस्थानों की अवधारणा विकसित की। इन विश्वविद्यालयों में भारत ही नहीं, बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और दक्षिण-पूर्व एशिया से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। आधुनिक विश्वविद्यालयों जैसे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और एमआईटी में भी यही अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण देखने को मिलता है, जहाँ दुनिया भर के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। 2. अनुसंधान आधारित शिक्षा प्रणाली बौद्ध शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान और तार्किक विचार-विमर्श को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था। विद्यार्थी केवल गुरु के ज्ञान को ग्रहण नहीं करते थे, बल्कि शास्त्रार्थ, तर्क-वितर्क और बौद्धिक बहस के माध्यम से ज्ञान को परिष्कृत करते थे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी शोध-अध्ययन, आलोचनात्मक चिंतन और स्वतंत्र विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है, जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली से प्रेरित माना जा सकता है। 3. नैतिक शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य बौद्ध शिक्षा में नैतिकता, अनुशासन, करुणा और आत्मचिंतन का महत्वपूर्ण स्थान था। विद्यार्थियों को केवल बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं कराया जाता था, बल्कि ध्यान (मेडिटेशन) और मानसिक एकाग्रता के अभ्यास भी करवाए जाते थे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी मानसिक स्वास्थ्य और माइंडफुलनेस (Mindfulness) को अत्यधिक महत्त्व दिया जाने लगा है। कई विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान अब तनाव प्रबंधन, ध्यान और योग को शिक्षा प्रणाली में शामिल कर रहे हैं। विशेष रूप से पश्चिमी देशों में माइंडफुलनेस आधारित शिक्षा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। 4. समावेशी और लोकतांत्रिक शिक्षा बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक पृष्ठभूमि का भेदभाव नहीं था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में सभी वर्गों के विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान किए जाते थे। यह समावेशी दृष्टिकोण आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी देखने को मिलता है, जहाँ विविध सांस्कृतिक और सामाजिक समूहों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने पर बल दिया जाता है। आज की शिक्षा नीति भी समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने पर बल देती है, जो बौद्ध परंपरा से प्रेरित हो सकती है। 5. बौद्ध अध्ययन और पुनरुद्धार भारत में बौद्ध शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्धार के प्रयास आज भी जारी हैं। 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया गया, जो यह दर्शाता है कि बौद्ध शिक्षा पद्धति और उसके मूल्यों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह विश्वविद्यालय एक वैश्विक संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ बहु-विषयक अध्ययन को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न देशों में बौद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ प्राचीन बौद्ध शिक्षाओं का अध्ययन किया जाता है। 6. पर्यावरण शिक्षा और सतत विकास बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने पर बल दिया जाता था। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शिक्षा दी थी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास (Sustainable Development) को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दुनिया भर के विश्वविद्यालय अब पर्यावरण अध्ययन, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से जुड़े पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दे रहे हैं। 7. बौद्ध शिक्षा के सिद्धांत और शिक्षण विधियाँ बौद्ध शिक्षा में अनुभवजन्य अध्ययन (Experiential Learning) और व्यावहारिक शिक्षा (Practical Learning) पर बल दिया जाता था। आज की शिक्षा प्रणाली में भी व्यावहारिक शिक्षण, केस स्टडीज, प्रोजेक्ट-आधारित अध्ययन और प्रयोगशाला कार्य जैसी विधियाँ अपनाई जा रही हैं, जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली से प्रभावित प्रतीत होती हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित न होकर समाज और व्यक्ति के समग्र विकास का माध्यम रही है। इसकी शिक्षाएँ आज भी नैतिकता, शांति, पर्यावरण संरक्षण, और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रासंगिक हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बौद्ध शिक्षा के मूल सिद्धांतों को अपनाकर एक अधिक नैतिक, समावेशी और शोध-आधारित शिक्षण प्रणाली का निर्माण किया जा सकता है। अतः, यह आवश्यक है कि हम बौद्ध शिक्षा केंद्रों के मूल्यों को पुनः स्थापित कर उन्हें समकालीन शिक्षा प्रणाली में अधिक प्रभावी रूप से समाहित करने का प्रयास करें। निष्कर्ष बौद्ध शिक्षा केंद्रों ने केवल भारत के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान नहीं दिया, बल्कि संपूर्ण एशिया और विश्व में ज्ञान के प्रसार को भी बढ़ावा दिया। इन प्राचीन विश्वविद्यालयों में व्याप्त समावेशिता, अनुसंधान-आधारित अध्ययन, नैतिक शिक्षा, और वैश्विक दृष्टिकोण आधुनिक शिक्षा प्रणाली के कई पहलुओं को प्रभावित करते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में तार्किक चिंतन, स्वतंत्र विचार और आलोचनात्मक विश्लेषण को प्रोत्साहित किया जाता था। यह परंपरा आधुनिक शोध पद्धतियों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान और नवाचार पर बढ़ता हुआ जोर, अकादमिक स्वतंत्रता और संवादात्मक शिक्षण पद्धतियाँ बौद्ध शिक्षा की ही देन हैं। इसके अतिरिक्त, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में नैतिकता और मानसिक अनुशासन को अत्यधिक महत्त्व दिया गया था। आज, जब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल व्यावसायिक सफलता प्राप्त करना बनता जा रहा है, तब बौद्ध शिक्षा की मूल भावना—नैतिकता, करुणा, और सामाजिक उत्तरदायित्व—को पुनः अपनाने की आवश्यकता है। माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी प्राचीन शिक्षाएँ अब वैश्विक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बन रही हैं, जिससे विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन देखा जा सकता है। बौद्ध शिक्षा केंद्रों की समावेशीता और लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली भी आधुनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जाति, धर्म, या सामाजिक पृष्ठभूमि के भेदभाव से मुक्त शिक्षा व्यवस्था की जो अवधारणा इन प्राचीन केंद्रों में थी, वही आज की वैश्विक शिक्षा प्रणाली में समानता और समावेशिता के रूप में देखी जाती है। आज, जब शिक्षा प्रणाली तेजी से डिजिटल हो रही है और तकनीकी नवाचार शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं, तब भी बौद्ध शिक्षा की मूल शिक्षण पद्धतियाँ—व्यावहारिक शिक्षा, संवाद आधारित अध्ययन, और अनुभवजन्य शिक्षण—प्रासंगिक बनी हुई हैं। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में भी बौद्ध दर्शन की शिक्षाएँ आधुनिक पाठ्यक्रमों में अपना स्थान बना रही हैं। अतः, यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली केवल प्राचीन भारत की धरोहर नहीं है, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। यदि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बौद्ध शिक्षा के मूल तत्वों को पुनः अपनाया जाए, तो यह न केवल शिक्षा को अधिक नैतिक, वैज्ञानिक और समावेशी बनाएगा, बल्कि संपूर्ण समाज में ज्ञान, शांति और समृद्धि की स्थापना करने में भी सहायक सिद्ध होगा। संदर्भ 1. रोमिला थापर, प्राचीन भारत का इतिहास, दिल्ली: पेंगुइन बुक्स, 2014, पृष्ठ 210-225। 2. विनय कुमार, भारतीय शिक्षा प्रणाली में बौद्ध परंपरा का योगदान, मुंबई: सह्याद्रि प्रकाशन, 2012, पृष्ठ 99-112। 3. ताशी दोरजी, तिब्बती बौद्ध शिक्षा और उसका प्रभाव, धर्मशाला: बौद्ध अध्ययन संस्थान, 2018, पृष्ठ 132-148। 4. ए.एल. बाशम, भारत का सांस्कृतिक इतिहास, दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास, 1998, पृष्ठ 275-290। 5. नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुद्धार समिति रिपोर्ट, 2014, नालंदा विश्वविद्यालय: इतिहास और पुनरुद्धार की दिशा में प्रयास, पृष्ठ 5-20। 6. भदंत आनंद कौसल्यायन. (2017). बुद्ध और बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ. वाराणसी: महाबोधि पब्लिकेशन। 7. Barua, B. (1921). A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy. Calcutta: University of Calcutta. 8. Schumann, H. W. (2004). The Historical Buddha: The Times, Life, and Teachings of the Founder of Buddhism. Motilal Banarsidass Publishers. 9. Jataka Tales. (2002). Buddhist Literature and Education. Oxford: Oxford University Press. 10. Singh, L. (2015). Buddhist Education in India and its Global Influence. New Delhi: Wisdom Press. 11. Gombrich, R. (2006). Theravāda Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo. Routledge. |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 16, Issue 1, January-June 2025 |
| Published On | 2025-03-03 |
| Cite This | बौद्ध शिक्षा केंद्रों की ऐतिहासिक भूमिका एवं वर्तमान शिक्षा पर उनका प्रभाव - राजेंद्र मीणा, डॉ चंद्रशेखर शर्मा - IJAIDR Volume 16, Issue 1, January-June 2025. |
Share this

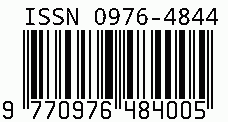
CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJAIDR DOI prefix is
10.71097/IJAIDR
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

