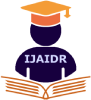
Journal of Advances in Developmental Research
E-ISSN: 0976-4844
•
Impact Factor: 9.71
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 16 Issue 1
2025
Indexing Partners
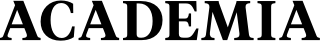




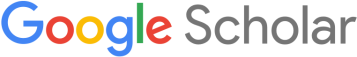








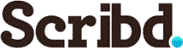




सामन्तवाद का उदय एवं पतन एक अध्ययन के रूप में
| Author(s) | चन्द्रप्रकाश कारपेंटर |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | सामन्तवाद का अर्थ - सामन्त तन्त्र अथवा सामन्तवाद जिसे अंग्रेजी भाषा में "फ्यूडेलिज्म" कहा जाता है, मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास की एक प्रमुख विशेषता रही है; क्योंकि उस युग की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएँ इसी सामन्त तन्त्र के आधार पर टिकी हुई थीं। इतिहासकार विलंडूरा के शब्दों में, "इतिहास की अधिकांश आर्थिक और सामाजिक रचनाओं के समान सामन्त तन्त्र भी स्थान, समय और मानव स्वभाव की आवश्यकताओं के अनुकूल था।" आज हमें यह प्रथा भले ही अनुचित लगे, परन्तु अपने आरम्भिक काल में सामन्त प्रथा न्यायसंगत एवं उचित होने के साथ-साथ कल्याणकारी भी रही थी। प्लैट एवं ड्रमंड के अनुसार, "जिस जमीन या स्वत्व पर अपने से ऊपर की किसी शक्ति को शुल्क देना पड़ता है, वह क्षेत्र "फ्यूड" कहलाता था। ऐसे एक या अनेक क्षेत्रों का मालिक "फ्यूडल लार्ड" कहलाता था।" फ्यूडल लार्ड के लिये हिन्दी में सामान्यतः "सामन्त" शब्द और उनकी परम्परा या प्रणाली के लिये "सामन्त तन्त्र" शब्द का प्रचलन हुआ है। सामन्तवाद का उदय : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - सामन्त-तन्त्र का जन्म किसी शासक की आज्ञा अथवा कुछ व्यक्तियों के संयुक्त प्रयास की उपज नहीं था। इसकी उत्पत्ति अपने आप स्वाभाविक रूप से हुई थी। पाँचवीं सदी के आरम्भ में जब रोमन साम्राज्य खण्ड-खण्ड होकर लड़खड़ाने लग गया तो सम्पूर्ण यूरोप अराजकता एवं अव्यवस्था में डूब गया। रोमन साम्राज्य को पूर्व और उत्तर की दिशाओं से बर्बर लुटेरे समूहों ने रौंद डाला। ये बर्बर लोग भारत-यूरोपीय मूल की भाषाएँ बोलने वाले बहुत से जर्मन कबीले थे, जो रोमन साम्राज्य की सीमा से दूर उत्तर सागर से कृष्ण सागर तक के क्षेत्र में घूमते-फिरते थे। ये जर्मन लोग "ट्यूटन" या "गौथ" नाम से भी पुकारे जाते थे। इन जर्मन कबीलों पर हूणों ने धावा बोला था। हूण लोग मध्य एशिया के यायावर घुड़सवार थे। चीन के हानवंशी शासकों ने हूणों को मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। इस प्रकार, चीनी लोगों ने हूणों को खदेड़ा, हूणों ने जर्मन कबीलों को खदेड़ा और जर्मन लोग भागकर रोमन साम्राज्य में घुसने लगे। इसलिये कई विद्वान् यह कहते हैं कि जर्मन लोगों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किया था, अपितु वे आश्रय की तलाश में रोमन साम्राज्य में घुस आये हैं। चौथी शताब्दी के अन्तिम काल में लगभग दो लाख जर्मनों (विसि गौथों अथवा पश्चिमी गौथों) ने डेन्यूब नदी को पारकर रोमन साम्राज्य में प्रवेश किया। रोमन सम्राट ने उन्हें हूणों से सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया, परन्तु यह शर्त भी रखी कि उन लोगों को रोमन सैनिक बनकर लड़ना पड़ेगा। परन्तु कुछ दिनों बाद ही रोमन अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार से पीड़ित होकर जर्मन लोगों ने विद्रोह कर दिया और 378 ई. में एड्रियानोपल के युद्ध में रोमनों को बुरी तरह से पराजित किया। युद्ध में प्राप्त सफलता से जर्मनों का उत्साह बढ़ गया और वे रोमन साम्राज्य पर टूट पड़े। 410 ई. में रोम पर भी उनका अधिकार हो गया। रोम से जर्मनों ने दक्षिणी फ्रांस और स्पेन पर धावा मारना शुरू किया और इन क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार जमा लिया। विसिगौथों के अलावा अन्य जर्मन कबीलों ने भी रोमन साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कायम कर लिया। ये जर्मन कबीले आपस में भी लड़ते रहते थे। उदाहरणार्थ, स्पेन में वांडाल (जर्मन कबीले का नाम) विसिगौथों से लड़े थे और 455 ई. वाडोलों ने भी रोम को लूटा था। 476 ई. में एक अन्य जर्मन सेनापति ओडोआचार ने अन्तिम रोमन सम्राट को सिंहासन से हटाकर स्वयं रोम का शासक बन बैठा। 500 ई. के आस-पास पूर्वी गौथों (औस्ट्रो गौथों) के नेता थियोडोरिक ने ओडोआचार को मारकर रोम के सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। 568 ई. में एक अन्य जर्मन कबीले " लोम्बार्ड" ने उत्तरी इटली पर आक्रमण कर उस क्षेत्र को जीत लिया। नवीं और दसवीं शताब्दियों में स्कैंडिनेविया (आजकल का नार्वे, स्वीडन और डेन्मार्क) में रहने वाली अर्द्ध सभ्य जर्मन जातियों ने यूरोप के कई भागों पर आक्रमण किये। उन्हें "नौर्थमेन" (उत्तरी मनुष्य) के नाम से पुकारा जाता था। इन लोगों ने इंगलैण्ड, आयरलैण्ड, फ्रांस के नोर्मन प्रदेश, रूस, दक्षिणी इटली, सिसली, फिनलैण्ड आदि अनेक क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य स्थापित किये। ईसाई धर्म स्वीकार करने के पूर्व नौर्थमेन पाशविक युद्धों और स्त्रियों तथा बच्चों को मारने में गौरव का अनुभव करते थे। उनकी लूट-खसोट तथा तोड-फोड़ से रोम की सांस्कृतिक उन्नति को गहरा आघात पहुँचा। रोमन साम्राज्य में आने वाली सभी जर्मन जातियों में सबसे अधिक प्रगतिशील फ्रैंक लोग थे, जिन्होंने अपने नेता क्लोविस (465-511 ई.) के नेतृत्व में सम्पूर्ण गाल (आज का फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैण्ड और पश्चिमी जर्मनी) पर अधिकार जमा लिया। क्लोविस के उत्तराधिकारी कमजोर निकले और राजभवन के प्रधान अधिकारी (जिसे "मेयर" कहा जाता था) पेपिन ने राजसत्ता हथिया ली। पेपिन का पुत्र शार्लमेन (अंग्रेजी में चार्ल्स महान्) बड़ा प्रतापी शासक हुआ। उसने 768 से 814 ई. तक शासन किया। उसका विशाल साम्राज्य उत्तरी सागर से इटली के मध्य तक और अन्ध महासागर से एल्ब नदी तक फैला हुआ था। चूँकि इस विशाल साम्राज्य पर एक व्यक्ति अकेला शासन नहीं कर सकता था, अतः शार्लमेन ने अपने युद्ध अभियानों में सहायता देने वालों को बड़े-बड़े भूमि खण्ड दिये, जिन पर उन्हें शासन करना था। इन भूमि खण्डों को "काउण्टी", "इची" और " मार्क्स" कहा जाता था और इनके शासकों को क्रमशः "काउण्ट", "ड्यूक" तथा "मार्किवस" कहा जाने लगा। इस प्रथा के कारण लोगों के पास बड़ी-बड़ी भू-सम्पत्तियाँ बन गईं और किसान अपने भूमि-स्वामित्व से वंचित हो गये। शार्लमेन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में एकता न रही और उसका विशाल साम्म्राज्य तीन प्रमुख राज्यों- जर्मनी, फ्रांस और इटली में विभाजित हो गया। इसी समय इन राज्यों पर बंजारे स्लाव लोगों, स्पेनं के मूर लोगों और उत्तरवासियों के आक्रमण शुरू हो गये जिससे पुनः अव्यवस्था फैल गई। राजाओं को अपने राज्यों पर नियन्त्रण रखना कठिन हो गया। सामन्तों के बीच आपसी लड़ाइयाँ बढ़ गई और बाहरी आक्रमणों ने लोगों का जीना ही मुश्किल कर दिया। इस सन्दर्भ में एच. जी. वेल्स ने लिखा है कि, "उस समय के संसार के हालात की कल्पना करना सामन्तवाद का विकास- सामन्तवाद जीवन का वह मार्ग था जो शार्लमेन के बाद के काल की विशिष्ट परिस्थितियों में अपनाया गया था। मूलतः यह भूमि की पट्टेदारी (स्वामित्व) पर आधारित एक सरकार का स्वरूप तथा एक आर्थिक पद्धति- दोनों ही था। परन्तु जबकि स्वयं सामन्तवाद में एक विशिष्ट प्रकार की समानता का विकास हुआ। सामन्ती प्रथाएँ एक स्थान से दूसरे स्थान, और भिन्न-भिन्न समयों में अलग-अलग स्वरूप धारण करती रहीं। इसलिए आगे के पृष्ठों में जिस सामन्तवाद का उल्लेख किया गया है उसे केवल पश्चिमी यूरोप के सामन्त-तन्त्र की सामान्य विशेषताएँ समझना ठीक रहेगा। सामन्तवाद का विकास भिन्न-भिन्न कालों की आवश्यकताओं के अनुकूल संशोधित रोमन, जर्मन और शायद सेल्टिक प्रथाओं से हुआ। इस समूचे विकास क्रम में दो प्रकार के सम्बन्धों का विशेष महत्त्व बना रहा (1) मनुष्य और मनुष्य के मध्य व्यक्तिगत सम्बन्ध, और (2) भूमि की पट्टेदारी अथवा भूमि का स्वामित्व। सैनिक सेवा पर आधारित मनुष्यों के मध्य सम्मानजनक सम्बन्धों वाली "वासलेज" नामक संस्था पहले प्रकार के सम्बन्ध को उजागर करती है। यद्यपि वासलेज का जन्म विवादाग्रस्त है, परन्तु सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि शार्लमेन के उत्तराधिकारियों के काल में "वासल" (अनुचर) का अभिप्राय अपने से ऊँचे व्यक्ति के अन्तर्गत लड़ने वाले व्यवसायी व्यक्ति से था। इस बीच, बिशप और काउण्ट जैसे अन्य बहुत से प्रभावशाली लोग जिनके अधिकार में बड़े-बड़े भूमि खण्ड थे, "फीडलस" अथवा "होमीनेज" (स्वामी भक्त) के रूप में राजा के साथ सम्बन्धित हो गये। बाद में शार्लमेन के उत्तराधिकारियों ने यह अनुभव किया कि मुसलमानों का मुकाबला करने के लिये एक सुसंगठित अश्वारोही सेना की आवश्यकता है, अतः वासल को घोड़ा रखने और सैनिक सेवा देने के बदले में भूमि का विशेष अनुदान दिया गया। इस प्रकार का अनुदान "बेनीफिस" कहलाता था और अनुदान में दी गई भूमि से वासल अपना तथा अपने घोड़े का खर्चा सरलता से पूरा कर सकता था। बाद में, सभी भूमिपतियों और प्रभावशाली लोगों से भी सैनिक सहयोग की अपेक्षा की जाने लगी। समय के साथ-साथ ये परम्पराएँ कानून का रूप ले बैठीं और तब इनसे सम्बन्धित समारोहों पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा। अपने स्वामी का" आदमी" (होमो) बनने के लिये वासल (अनुचर) को स्वामिभक्ति के कुछ कार्य सम्पादित करने पड़ते थे। चूँकि उसकी स्वामिभक्ति ही मुख्य बात थी, अतः उसे अपने स्वामी के प्रति "स्वामिभक्ति" की शपथ भी लेनी पड़ती थी। |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 16, Issue 1, January-June 2025 |
| Published On | 2025-03-08 |
| Cite This | सामन्तवाद का उदय एवं पतन एक अध्ययन के रूप में - चन्द्रप्रकाश कारपेंटर - IJAIDR Volume 16, Issue 1, January-June 2025. |
Share this

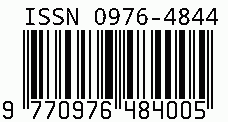
CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJAIDR DOI prefix is
10.71097/IJAIDR
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

