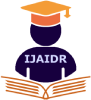
Journal of Advances in Developmental Research
E-ISSN: 0976-4844
•
Impact Factor: 9.71
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 16 Issue 1
2025
Indexing Partners
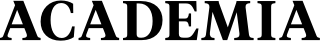




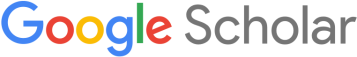








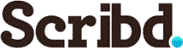




सम्राट अशोक की धम्म नीति की वर्तमान ऐतिहासिक प्रासंगिकता
| Author(s) | Pankaj Kumar Shukla |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महान और दूरदर्शी शासकों में से एक थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से एक समावेशी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। अशोक का धम्म उनकी शासन नीति का केंद्रीय तत्व था, जो बौद्ध धर्म से प्रेरित होते हुए भी किसी एक धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि एक सार्वभौमिक नैतिक आचार संहिता के रूप में उभरा। उनके शासन का उद्देश्य केवल सैन्य विस्तार और साम्राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करना नहीं था, बल्कि उन्होंने नैतिकता, करुणा, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। अशोक की शासकीय नीतियाँ कुशल प्रशासन, सामाजिक न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याणकारी योजनाओं का संतुलित मिश्रण थीं। उन्होंने प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ नैतिक मूल्यों को राज्य व्यवस्था में समाहित किया, जिससे उनके साम्राज्य में समृद्धि और शांति का माहौल बना। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और उन्होंने हिंसा की नीति त्यागकर धम्म के सिद्धांतों को अपनाया। इस परिवर्तन ने न केवल उनके शासन के स्वरूप को बदला, बल्कि उनके द्वारा प्रचारित नीतियों का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पड़ा। अशोक के धम्म की शिक्षाएँ और उनकी नीतियाँ केवल धार्मिक सुधारों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने जनता के कल्याण के लिए चिकित्सा, शिक्षा, जल प्रबंधन, यातायात और कृषि के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार किए। उनके शिलालेखों से स्पष्ट होता है कि वे जनता की भलाई और न्यायसंगत शासन को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने न्यायिक प्रणाली को अधिक संवेदनशील और नैतिक बनाया तथा जनता की समस्याओं को समझने के लिए अधिकारियों को अधिक उत्तरदायी बनाया। यह शोध पत्र अशोक के धम्म और उनकी शासकीय नीतियों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेगा, जिससे यह समझा जा सके कि उनकी नीतियों ने भारतीय प्रशासन, समाज और सांस्कृतिक मूल्यों को कैसे प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन इस बात पर भी प्रकाश डालेगा कि अशोक की नीतियाँ आज के संदर्भ में कितनी प्रासंगिक हैं और किस प्रकार उनके विचार वर्तमान समाज और शासन प्रणाली के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। अशोक का धम्म: एक नैतिक संहिता अशोक के धम्म को केवल धार्मिक अवधारणा तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह एक व्यापक नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन था, जिसका उद्देश्य साम्राज्य में शांति, समरसता और नैतिकता को स्थापित करना था। धम्म किसी विशिष्ट धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि यह एक सार्वभौमिक नैतिक संहिता थी, जो मानवता के कल्याण पर आधारित थी। अशोक ने अपने शिलालेखों के माध्यम से धम्म के सिद्धांतों को स्पष्ट किया और इन्हें प्रशासनिक और सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग बनाया। उनका धम्म व्यक्तिगत आचरण, पारिवारिक जीवन, सामाजिक दायित्व और शासकीय नीति को एकरूपता में बांधने का प्रयास था। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं— 1. सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता: अशोक ने धार्मिक समरसता को अपने धम्म का एक महत्वपूर्ण आधार बनाया। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान और समानता का भाव रखा और अपने शिलालेखों के माध्यम से यह संदेश दिया कि किसी भी धर्म के अनुयायियों को नीचा नहीं समझना चाहिए। उनके अनुसार, सभी धार्मिक परंपराएँ नैतिकता, सत्य और अहिंसा का उपदेश देती हैं, इसलिए किसी भी धर्म को श्रेष्ठ या हीन मानने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति आदरभाव बनाए रखें और धार्मिक मतभेदों को बढ़ावा न दें। 2. अहिंसा और दयालुता: कलिंग युद्ध की विभीषिका देखने के बाद अशोक ने अहिंसा को अपने धम्म का केंद्रीय सिद्धांत बनाया। उन्होंने न केवल युद्ध से दूरी बनाई, बल्कि जीवों के प्रति करुणा और दया का संदेश भी दिया। उन्होंने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया और अपने शिलालेखों में यह घोषणा की कि उनके शासनकाल में कम से कम हिंसा होनी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार किए ताकि मानव और पशु दोनों का कल्याण हो सके। 3. सामाजिक नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों का प्रचार: अशोक ने अपने धम्म में सामाजिक नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों को भी विशेष स्थान दिया। उन्होंने माता-पिता की सेवा, गुरुजनों के प्रति सम्मान, वृद्धों की देखभाल, पड़ोसियों के प्रति सद्भाव और सत्य बोलने जैसी नैतिक शिक्षाओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे क्रोध, द्वेष और स्वार्थ जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचें और समाज में सद्भाव बनाए रखें। 4. राज्य में नैतिकता का प्रसार: अशोक ने प्रशासन में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जो समाज में नैतिकता और धर्मपरायणता को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थे। इन महामात्रों का कार्य केवल धम्म का प्रचार ही नहीं था, बल्कि वे जनता की समस्याओं को सुनने, गरीबों की सहायता करने और न्याय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए भी उत्तरदायी थे। इससे प्रशासनिक स्तर पर भी नैतिकता को बल मिला। 5. सार्वजनिक कल्याण और सेवा: अशोक ने अपने धम्म के अंतर्गत जनता के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने अस्पतालों, कुओं, सड़कों, विश्रामगृहों और पौधारोपण की व्यवस्था करवाई, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिला। उन्होंने न केवल मनुष्यों के लिए, बल्कि पशुओं के लिए भी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाईं। उनके शासनकाल में व्यापारी, तीर्थयात्री और साधु-संतों के लिए सरायों और सुरक्षित मार्गों की व्यवस्था की गई। अशोक का धम्म केवल धार्मिक शिक्षाओं का संग्रह नहीं था, बल्कि यह नैतिकता, सहिष्णुता और लोक कल्याण पर आधारित एक व्यावहारिक नीति थी। यह नीति उनके प्रशासन, न्याय प्रणाली, सामाजिक सुधारों और जनकल्याणकारी योजनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने अपने धम्म के माध्यम से सम्राट और प्रजा के संबंधों को अधिक नैतिक और मानवीय बनाने की कोशिश की। अशोक का धम्म आज भी एक आदर्श सामाजिक दर्शन के रूप में प्रासंगिक बना हुआ है, जो सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की शिक्षा देता है। सम्राट अशोक की शासकीय नीति अशोक की शासन नीति केवल सैन्य शक्ति और प्रशासनिक दक्षता पर आधारित नहीं थी, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याण को भी प्रमुख स्थान दिया गया था। उनकी नीतियों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है: 1. प्रशासनिक व्यवस्था o अशोक ने प्रशासन को केंद्रीकृत और संगठित रूप में रखा। o उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में ‘राजुक’ (शासकीय अधिकारी) और ‘महामात्र’ (विशेष अधिकारी) नियुक्त किए, जो प्रशासन और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में सहायता करते थे। o उनके शिलालेखों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वे जनता के कल्याण हेतु अधिकारी नियुक्त करते थे। 2. न्याय और कानून व्यवस्था o अशोक ने निष्पक्ष न्याय प्रणाली को बढ़ावा दिया। o उनके आदेशों के अनुसार, दंड को न्यूनतम किया जाना चाहिए और अपराधियों को सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। o उन्होंने दासों और सेवकों के साथ उचित व्यवहार पर बल दिया। 3. धार्मिक सहिष्णुता और धर्म प्रचार o अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बावजूद किसी भी धर्म पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। o उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका, मध्य एशिया और मिस्र तक भेजा, जिससे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। o उनके अभिलेख बताते हैं कि उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की नीति अपनाई। 4. जन कल्याणकारी योजनाएँ o अशोक ने कृषि, सिंचाई और जल प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार किए। o उन्होंने अस्पतालों, सड़कों और सार्वजनिक विश्रामगृहों का निर्माण करवाया। o पशुओं के लिए भी चिकित्सा व्यवस्था की गई। 5. विदेश नीति और शांतिवाद o कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने आक्रामक युद्ध नीति को त्यागकर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को अपनाया। o उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रता बनाए रखने पर जोर दिया। अशोक की नीतियों का प्रभाव सम्राट अशोक की नीतियों ने भारतीय समाज, प्रशासन और सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला। उनका शासन केवल एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण तक सीमित नहीं था, बल्कि यह नैतिकता, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण की ओर उन्मुख था। अशोक के धम्म ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को समाप्त करने, कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएँ चलाईं। उनके प्रयासों से समाज में दया, करुणा और सेवा की भावना को प्रोत्साहन मिला, जिससे भारतीय समाज में नैतिकता और मानवीय मूल्यों को एक नई दिशा मिली। अशोक की विदेश नीति भी उनके धम्म के अनुरूप थी। उन्होंने अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए अपने दूतों को भेजा, जिससे भारत का सांस्कृतिक प्रभाव एशिया और अन्य देशों तक फैला। बौद्ध धर्म के प्रचारकों को श्रीलंका, म्यांमार, चीन और मध्य एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया, जिससे यह धर्म न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी प्रमुख आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांत के रूप में स्थापित हुआ। अशोक की नीतियों ने भारत को एक वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र बनाने में सहायता की और उनके संदेश ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनकी प्रशासनिक नीतियाँ भी अत्यधिक प्रभावशाली रहीं। उन्होंने साम्राज्य को संगठित करने के लिए उसे अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया और वहाँ योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनकल्याण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई, जिनका कार्य न केवल शासन व्यवस्था की देखरेख करना था, बल्कि जनता के कल्याण को भी सुनिश्चित करना था। उनकी इस प्रशासनिक प्रणाली के तत्व भारत की आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में भी परिलक्षित होते हैं, जहाँ कल्याणकारी योजनाओं, कानून व्यवस्था और नीति-निर्माण की प्रक्रिया में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने में भी अशोक की नीति अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया और किसी भी धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। उनके शिलालेखों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वे सभी धार्मिक परंपराओं को नैतिकता और सत्य की दृष्टि से समान मानते थे। यह नीति भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और बहुलतावाद की भावना से मेल खाती है। आज भी भारत की "विविधता में एकता" की भावना को सशक्त करने में अशोक के विचारों की महत्त्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अशोक की नीतियों का प्रभाव केवल उनके शासनकाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारत के ऐतिहासिक विकास में एक स्थायी धरोहर बन गया। उनके प्रशासनिक सुधार, जनकल्याणकारी योजनाएँ, धार्मिक सहिष्णुता और अहिंसा के सिद्धांत आज भी प्रेरणादायक हैं। उनकी धम्म नीति केवल धार्मिक नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक दर्शन था, जिसने भारतीय समाज और शासन व्यवस्था को एक नई दिशा दी। भारत की आधुनिक नीतियों में कहीं न कहीं अशोक की धम्म नीति की झलक देखी जा सकती है, जो समाज में शांति, समरसता और नैतिकता की स्थापना के लिए आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। निष्कर्ष सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे दूरदर्शी और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उनका शासन केवल विस्तारवाद पर केंद्रित नहीं था, बल्कि उन्होंने नैतिकता, सामाजिक समरसता और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दी। अशोक की धम्म नीति केवल धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक सुधार का आधार बनी। उन्होंने एक ऐसा शासन स्थापित किया जिसमें धर्म, नैतिकता और लोक कल्याण को सर्वोच्च स्थान दिया गया। अशोक की नीतियों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सार्वभौमिकता थी। वे केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने सभी धर्मों और समाज के सभी वर्गों को समान रूप से सम्मान दिया। धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समानता और लोक कल्याण की भावना उनके शासन की बुनियाद बनी। उन्होंने अहिंसा को केवल युद्धों से बचने का साधन नहीं माना, बल्कि इसे एक व्यापक जीवनशैली और प्रशासनिक नीति का रूप दिया। कलिंग युद्ध के बाद उनकी धम्म नीति और भी सशक्त हो गई, जिसमें उन्होंने अहिंसा, करुणा और परोपकार को समाज में स्थापित करने के लिए व्यापक प्रयास किए। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अशोक का शासन अत्यंत संगठित और जनकल्याणकारी था। उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जो जनता की समस्याओं का समाधान करने और धम्म के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यरत रहे। उन्होंने जल आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाओं, सड़कों, विश्रामगृहों और शिक्षा संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी, जिससे उनके राज्य में नागरिकों की भलाई सुनिश्चित हो सके। अशोक की विदेश नीति भी उनकी धम्म नीति के अनुरूप थी। उन्होंने शांति और मैत्रीपूर्ण संबंधों को महत्व दिया और विभिन्न देशों में अपने दूत भेजे ताकि बौद्ध धर्म और धम्म के सिद्धांतों का प्रचार किया जा सके। श्रीलंका, म्यांमार, चीन और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय भी काफी हद तक अशोक की नीतियों को जाता है। उनकी यह नीति भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में सहायक बनी। उनकी नीतियों का प्रभाव उनके शासनकाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका गहरा असर पड़ा। भारत के ऐतिहासिक और राजनीतिक विकास में अशोक की नीतियाँ एक स्थायी विरासत के रूप में देखी जाती हैं। आज भी भारत की बहुलतावादी संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की अवधारणा कहीं न कहीं अशोक की धम्म नीति से प्रेरित प्रतीत होती है। भारतीय संविधान में निहित धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समानता के सिद्धांत उनकी नीति की आधुनिक अभिव्यक्ति हैं। समकालीन समय में भी अशोक की धम्म नीति और उनकी प्रशासनिक नीतियाँ प्रासंगिक बनी हुई हैं। उनके विचार शांति, अहिंसा, सामाजिक कल्याण और नैतिकता को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकते हैं। प्रशासनिक कुशलता, नीति-निर्माण और धर्मनिरपेक्षता जैसे तत्व आज के लोकतांत्रिक शासन में भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। सम्राट अशोक का जीवन और उनकी नीतियाँ यह दर्शाती हैं कि एक सशक्त शासन केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि नैतिकता, सहिष्णुता और लोक कल्याण पर आधारित होता है। उनकी धम्म नीति और शासकीय दृष्टिकोण न केवल भारतीय इतिहास में, बल्कि विश्व इतिहास में भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। संदर्भ सूची 1. रोमिला थापर – अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज़ (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1998), पृष्ठ 102-135। 2. आर.सी. मजूमदार – एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया (मैकमिलन, 1973), पृष्ठ 210-245। 3. डी.एन. झा – एंशिएंट इंडिया: एन इंटरप्रिटेशन (मणोहर पब्लिकेशन्स, 2004), पृष्ठ 180-215। 4. के.ए. नीलकंठ शास्त्री – ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1975), पृष्ठ 95-120। 5. यदुनाथ सरकार – अशोक द ग्रेट (बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 1962), पृष्ठ 50-98। 6. अल्तेकर, ए.एस. – स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया (मोतिलाल बनारसीदास, 1949), पृष्ठ 130-175। 7. हर्मन कुल्के और डाइटमार रॉथरमुंड – ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया (रूटलेज, 2004), पृष्ठ 75-110। 8. यू.एन. घोषाल – स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1957), पृष्ठ 220-265। 9. बुद्ध प्रकाश – अशोकाज धम्म (स्टर्लिंग पब्लिशर्स, 1962), पृष्ठ 45-85। 10. विनय लाल – हिस्ट्री ऑफ इंडिया (पेंग्विन बुक्स, 2006), पृष्ठ 155-195। 11. पी.एन. चोपड़ा – भारत का प्राचीन इतिहास (नेशनल बुक ट्रस्ट, 1985), पृष्ठ 170-210। 12. ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत – सियू-की: बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड (अनुवाद: सैम्युएल बील, 1884), पृष्ठ 80-140। 13. राजा राधाकांत देव – भारतीय प्रशासन और मौर्य शासन (कोलकाता विश्वविद्यालय, 1930), पृष्ठ 115-160। 14. ए.एल. बाशम – द वंडर दैट वॉज इंडिया (सिडविक एंड जैक्सन, 1954), पृष्ठ 200-240। 15. दामोदर धर्मानंद कोसंबी – एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री (पॉपुलर प्रकाशन, 1956), पृष्ठ 145-180। |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 16, Issue 1, January-June 2025 |
| Published On | 2025-03-27 |
| Cite This | सम्राट अशोक की धम्म नीति की वर्तमान ऐतिहासिक प्रासंगिकता - Pankaj Kumar Shukla - IJAIDR Volume 16, Issue 1, January-June 2025. |
Share this

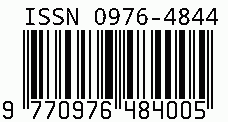
CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJAIDR DOI prefix is
10.71097/IJAIDR
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

