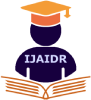
Journal of Advances in Developmental Research
E-ISSN: 0976-4844
•
Impact Factor: 9.71
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 16 Issue 1
2025
Indexing Partners
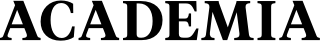




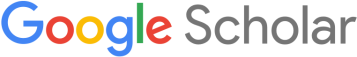








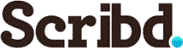




राजस्थान में वन संपदा का भौगोलिक विश्लेषण
| Author(s) | PREM SHANKAR KIRAR |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य, अपनी शुष्क जलवायु, विस्तृत मरुस्थलीय भूभाग, तथा भौगोलिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य पश्चिम में थार मरुस्थल से लेकर पूर्व में आर्द्रभूमि और घास के मैदानों तक फैला हुआ है, जिससे इसकी पारिस्थितिकी विविधतापूर्ण बनती है। भले ही राजस्थान का अधिकांश भाग शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु क्षेत्र में आता हो, फिर भी यहाँ वन संपदा का महत्वपूर्ण स्थान है। वन न केवल राज्य की पारिस्थितिकीय स्थिरता में योगदान देते हैं, बल्कि जैव विविधता संरक्षण, जल संतुलन, मिट्टी के कटाव को रोकने, तथा सामाजिक-आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान के वन मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला, हाडौती क्षेत्र, और कुछ नदियों के किनारों तक सीमित हैं। हालाँकि, राज्य में वनस्पतियों की विविधता जलवायु और मिट्टी के अनुसार अलग-अलग प्रकार की देखी जाती है। अरावली क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वनस्पति मिलती है, जबकि पश्चिमी भाग में कांटेदार झाड़ियाँ और रेत में उगने वाली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। राज्य के वनों में अनेक दुर्लभ वनस्पतियाँ और जीव-जंतु पाए जाते हैं, जो इसकी जैव विविधता को समृद्ध करते हैं। वन संसाधन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहाँ के वनों से तेंदू पत्ता, गोंद, औषधीय पौधे, लकड़ी, और चारे की आपूर्ति होती है, जिससे स्थानीय समुदायों को आजीविका प्राप्त होती है। साथ ही, राज्य के कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, जैसे कि रणथंभौर, सरिस्का, एवं मुकुंदरा हिल्स, पारिस्थितिकी संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। राजस्थान के वन जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ जल संकट एक गंभीर समस्या है। हालाँकि, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण, शहरीकरण, तथा कृषि के विस्तार के कारण राजस्थान के वन क्षेत्र पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। वन अतिक्रमण, अवैध कटाई, मरुस्थलीकरण, और जलवायु परिवर्तन जैसे कारक राज्य के वनों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और विभिन्न पर्यावरणीय संगठनों द्वारा वन संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। हरित राजस्थान योजना, संयुक्त वन प्रबंधन (JFM), तथा वृक्षारोपण अभियानों के माध्यम से वन क्षेत्र के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस शोध पत्र में राजस्थान के वन संसाधनों का भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें राज्य के वन आवरण, उनका वितरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकीय एवं आर्थिक महत्व, प्रमुख चुनौतियाँ, तथा वन संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन राजस्थान में वन संरक्षण की आवश्यकताओं को समझने और वनों के सतत प्रबंधन की दिशा में प्रभावी रणनीतियाँ विकसित करने में सहायक होगा। राजस्थान के वन आवरण एवं वितरण राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 9.57% (32,737 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र वन भूमि के अंतर्गत आता है। हालाँकि, राज्य का अधिकांश भाग शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु क्षेत्र में आता है, फिर भी यहाँ वनों की विविधता जलवायु, मिट्टी की उर्वरता, वर्षा और स्थलाकृतिक विशेषताओं के अनुसार बदलती रहती है। राजस्थान के वनों का वितरण असमान रूप से फैला हुआ है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला, हाडौती क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग और कुछ नदियों के किनारे महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों के रूप में देखे जाते हैं। वनस्पतियों के प्रकार और वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा, तापमान, मिट्टी की संरचना, और मानवीय हस्तक्षेप शामिल हैं। राजस्थान में वनों को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: 1. शुष्क पर्णपाती वन: ष्क पर्णपाती वन मुख्य रूप से अरावली पर्वत श्रृंखला, कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, तथा सिरोही जिलों में पाए जाते हैं। ये वन अपेक्षाकृत अधिक वर्षा (600-1000 मिमी प्रति वर्ष) वाले क्षेत्रों में स्थित हैं और यहाँ साल, धोक, शीशम, खैर, बेर, तथा बबूल जैसे वृक्षों की प्रचुरता देखने को मिलती है। ये वन वर्षा ऋतु में सघन दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिससे इन वनों की विशेष पहचान बनती है। इस क्षेत्र के जंगलों में बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, और चिंकारा जैसे वन्यजीव भी पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य और कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इसी प्रकार के वनों का हिस्सा हैं। 2. कांटेदार वन: राजस्थान के पश्चिमी भाग में, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 150-500 मिमी के बीच होती है, वहाँ मुख्य रूप से कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। इन वनों का विस्तार जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और नागौर जिलों में देखा जाता है। चूँकि यहाँ मिट्टी शुष्क और रेतीली होती है तथा पानी की उपलब्धता सीमित होती है, इसलिए इस क्षेत्र की वनस्पतियाँ अनुकूलित रूप में कांटेदार और गहरे जड़ वाले होते हैं। इन वनों में प्रमुख रूप से बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, सांगरी, कैर, तथा बेर जैसे पौधे पाए जाते हैं, जो कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। खेजड़ी का विशेष रूप से आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि यह न केवल चारागाह वनस्पति प्रदान करता है, बल्कि यह राजस्थान के ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी है। इन क्षेत्रों में वन्यजीवों की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियाँ भी देखी जाती हैं, जिनमें काला हिरण, लोमड़ी, गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड), और मरुस्थलीय सरीसृप शामिल हैं। यह क्षेत्र थार मरुस्थल का हिस्सा होने के कारण वनों के अत्यधिक विस्तार की संभावनाएँ सीमित हैं, लेकिन सरकारी प्रयासों और सामाजिक वृक्षारोपण कार्यक्रमों के माध्यम से वनस्पति संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। 3. नदी तटीय वन एवं दलदली वन: राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जहाँ नदियाँ बहती हैं, वहाँ जल की निरंतर उपलब्धता के कारण कुछ तटीय वन और दलदली वन भी देखने को मिलते हैं। ये वन मुख्य रूप से चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, और माही नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों में शीशम, अर्जुन, गूलर, जामुन, खैर, तथा सागौन प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये वन न केवल स्थानीय जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि जल संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। विशेष रूप से चंबल नदी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए, और विभिन्न प्रकार के जल पक्षियों के लिए आदर्श पर्यावास प्रदान करती हैं। इसी प्रकार, दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में स्थित दलदली वन कई प्रकार की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के लिए आश्रय स्थल का कार्य करते हैं। हालाँकि, इन क्षेत्रों में अतिक्रमण और खेती के विस्तार के कारण वनस्पतियों को खतरा भी बना रहता है। वन क्षेत्र का जिला-वार वितरण राजस्थान में वन क्षेत्र का वितरण सभी जिलों में समान रूप से नहीं है। राज्य के कुछ जिलों में अपेक्षाकृत अधिक वन क्षेत्र उपलब्ध है, जबकि कुछ जिलों में यह अत्यंत सीमित मात्रा में है। निम्नलिखित जिलों में सबसे अधिक वन आवरण पाया जाता है: 1. उदयपुर – अरावली पर्वतों की उपस्थिति के कारण यहाँ वन क्षेत्र काफी विकसित है। 2. सिरोही – यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में सघन वनस्पति पाई जाती है। 3. राजसमंद – यहाँ भी पर्याप्त मात्रा में जंगल मौजूद हैं। 4. चित्तौड़गढ़ – इस क्षेत्र में भी शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 5. कोटा और झालावाड़ – इन जिलों में भी अच्छी मात्रा में वन क्षेत्र उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर, जैसलमेर, बीकानेर, और चूरू जैसे पश्चिमी राजस्थान के जिले कम वर्षा और रेतीली मिट्टी के कारण न्यूनतम वन आवरण वाले क्षेत्र हैं। वन क्षेत्र की मात्रा में परिवर्तन वनों के संरक्षण के लिए सरकार और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा समय-समय पर वनीकरण परियोजनाएँ चलाई गई हैं, जिनका प्रभाव वन क्षेत्र की मात्रा पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हाल के वर्षों में राजस्थान में वनावरण दर (Forest Cover Rate) में वृद्धि दर्ज की गई है, हालाँकि यह वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी है। राजस्थान में वन आवरण सीमित होते हुए भी राज्य के पारिस्थितिकीय और आर्थिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वन वितरण का स्वरूप क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, तथा स्थलाकृतिक विशेषताओं पर निर्भर करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के वन विकसित हुए हैं। अरावली पर्वतीय क्षेत्र और हाडौती के हिस्सों में सघन वन क्षेत्र पाया जाता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पतियाँ अधिक प्रचलित हैं। हालाँकि, कृषि विस्तार, बढ़ती जनसंख्या, और औद्योगिकीकरण के कारण वन क्षेत्र पर दबाव बना हुआ है, जिससे वन संरक्षण की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। वनों के सतत विकास और संरक्षण के लिए आवश्यक है कि वनीकरण परियोजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए, जनभागीदारी को बढ़ाया जाए, तथा सरकारी नीतियों को और अधिक सख्ती से लागू किया जाए। इसके साथ ही, जल स्रोतों के संरक्षण और वृक्षारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर राज्य के वन क्षेत्र को संतुलित और सुदृढ़ किया जा सकता है। वन संपदा का आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय महत्व राजस्थान में वन संपदा न केवल आर्थिक गतिविधियों का आधार है, बल्कि यह राज्य के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ के वनों का उपयोग उद्योग, कृषि, पशुपालन, तथा विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इसके अलावा, वनों का संरक्षण जैव विविधता, जल संसाधनों और जलवायु संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। राज्य के वन क्षेत्र सीमित होते हुए भी पारिस्थितिकीय और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 1. जैव विविधता संरक्षण: राजस्थान के वन अनेक दुर्लभ और संकटग्रस्त जीव-जंतुओं तथा वनस्पतियों का निवास स्थल हैं। राज्य में स्थित प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, और माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य में समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। ये क्षेत्र बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, लोमड़ी, हिरण, चिंकारा, गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं। इसके अलावा, इन वनों में अनेक औषधीय और उपयोगी पौधे भी पाए जाते हैं, जिनका पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग किया जाता है। जैव विविधता का संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। 2. वन उत्पादों का आर्थिक महत्व: राजस्थान के वनों से अनेक प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनमें शामिल हैं: • लकड़ी और ईंधन – राजस्थान के वनों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग निर्माण कार्यों, कृषि उपकरणों, और घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। • गोंद और तेंदू पत्ता – राज्य में गोंद उत्पादन महत्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधि है, जो विशेष रूप से दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के वनों में किया जाता है। तेंदू पत्ते का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। • औषधीय पौधे – राजस्थान के वनों में अश्वगंधा, गुग्गल, आँवला, ब्राह्मी, और अर्जुन जैसे अनेक औषधीय पौधे पाए जाते हैं, जो आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों में प्रयोग किए जाते हैं। • चारागाह और चारा उत्पादन – राजस्थान का पशुपालन उद्योग काफी हद तक वनों पर निर्भर करता है। खेजड़ी, बेर, सांगरी, तथा बबूल जैसे वृक्षों से प्राप्त चारा पशुओं के लिए महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इन उत्पादों के व्यवसाय से अनेक ग्रामीण समुदायों को रोजगार मिलता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी सहयोग मिलता है। 3. जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण: राजस्थान के वन क्षेत्र जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से अरावली पर्वतमाला में स्थित वनस्पति जलग्रहण क्षेत्रों के रूप में कार्य करती है, जिससे नदियों, झीलों और भूमिगत जल स्रोतों को पुनर्भरण मिलता है। • वनस्पति आवरण वर्षा जल को संचित करने में मदद करता है, जिससे जलस्तर गिरने से रोका जा सकता है। • नदी तटीय वन और दलदली वन प्राकृतिक जलाशयों के रूप में कार्य करते हैं और जल स्रोतों को संरक्षित रखते हैं। • राजस्थान में बिसलपुर, माही बजाज सागर, और जवाई बांध जैसे जलाशयों की स्थिरता में भी वनों की अहम भूमिका होती है। जल संरक्षण की यह प्रक्रिया न केवल पीने और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को बढ़ाती है, बल्कि राज्य में सतत कृषि और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होती है। 4. मिट्टी अपरदन की रोकथाम एवं मरुस्थलीकरण नियंत्रण: राजस्थान के वन क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण कार्य मिट्टी अपरदन को रोकना और मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना है। राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित रेगिस्तानी जिलों में वृक्षारोपण परियोजनाएँ तथा वन संरक्षण नीतियाँ मरुस्थलीकरण की गति को धीमा करने में मदद कर रही हैं। • पेड़-पौधे जड़ों के माध्यम से मिट्टी को बाँध कर रखते हैं, जिससे तेज़ हवाओं और पानी के कारण मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। • खेजड़ी, बबूल, और रोहिड़ा जैसे वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं, जो मिट्टी की नमी को संरक्षित रखने में सहायक होती हैं। • थार मरुस्थल क्षेत्र में किए गए वृक्षारोपण कार्यक्रमों से मिट्टी के कटाव को कम करने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सफलता मिली है। इन प्रयासों से राजस्थान के कई क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिली है, जिससे कृषि योग्य भूमि को बचाया जा सका है। 5. पर्यावरणीय लाभ: वन पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में वन संपदा निम्नलिखित पर्यावरणीय लाभ प्रदान करती है: • कार्बन अवशोषण – राजस्थान के वनों में मौजूद वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं। • वायुमंडल को शुद्ध करना – पेड़-पौधे प्रदूषकों को अवशोषित करके वायुमंडल को स्वच्छ बनाते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होता है। • वर्षा संतुलन बनाए रखना – अरावली पर्वतमाला के वनों से होने वाला वाष्पीकरण और वायुमंडलीय नमी का संतुलन राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा चक्र को प्रभावित करता है। • तापमान को नियंत्रित करना – वन क्षेत्र स्थानीय जलवायु को ठंडा बनाए रखते हैं और अत्यधिक तापमान को कम करने में मदद करते हैं। वनों के ये पर्यावरणीय लाभ राज्य के पारिस्थितिकीय तंत्र को बनाए रखने और जीवन को अधिक अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान के वन संसाधन आर्थिक और पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ये वन न केवल राज्य के जैव विविधता को सुरक्षित रखने में सहायक हैं, बल्कि अनेक प्रकार के वनोपज, औषधीय पौधों, और चारागाहों के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी समर्थन देते हैं। इसके अलावा, वन पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, जल संरक्षण, मिट्टी अपरदन की रोकथाम, तथा मरुस्थलीकरण नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, वन क्षेत्र पर बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप, अवैध कटाई, और शहरीकरण जैसी चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और स्थानीय समुदायों को मिलकर वन संरक्षण कार्यक्रमों, वृक्षारोपण अभियानों, और सतत विकास की रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। वन संरक्षण से न केवल पर्यावरणीय लाभ होंगे, बल्कि राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान में वन संसाधनों की चुनौतियाँ राजस्थान, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ वन क्षेत्र सीमित होते हुए भी राज्य के पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, राजस्थान के वन संसाधनों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी सततता और दीर्घकालिक संरक्षण प्रभावित हो रहा है। ये चुनौतियाँ प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारकों से जुड़ी हुई हैं। 1. वृक्ष कटाई और अतिक्रमण: राजस्थान में कृषि विस्तार, शहरीकरण, और बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है। • जनसंख्या वृद्धि के कारण वन भूमि पर अतिक्रमण बढ़ रहा है, जिससे प्राकृतिक वनों का क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है। • खेती के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे वन क्षेत्र और जैव विविधता को भारी नुकसान हो रहा है। • खनन गतिविधियाँ, विशेष रूप से अरावली पर्वतमाला में, वन संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। • लकड़ी, जलावन और निर्माण कार्यों में उपयोग के लिए अवैध कटाई की समस्या भी बढ़ती जा रही है। वनों की अवैध कटाई से न केवल जैव विविधता को खतरा होता है, बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन और जलवायु परिवर्तन की समस्याएँ भी बढ़ती हैं। 2. मरुस्थलीकरण एवं जलवायु परिवर्तन: राजस्थान में जलवायु परिवर्तन और मानवजनित गतिविधियों के कारण मरुस्थलीकरण की समस्या तेजी से बढ़ रही है। • वर्षा की कमी और अनियमितता के कारण वन क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं और वनस्पतियों का प्राकृतिक पुनर्जनन बाधित हो रहा है। • थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के पश्चिमी जिलों में हो रहा है, जिससे वन क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। • तेज़ हवाओं और अपर्याप्त वनस्पति आवरण के कारण मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, जिससे वन भूमि बंजर हो रही है। • जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे वन्य जीव-जंतुओं और पौधों की प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने और वन क्षेत्र को संरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, जल संरक्षण और जैव विविधता प्रबंधन की आवश्यकता है। 3. चरागाही दबाव और अतिक्रमण: राजस्थान में पशुपालन एक प्रमुख आजीविका का साधन है, लेकिन अत्यधिक पशुधन के कारण वन क्षेत्र पर चरागाही दबाव लगातार बढ़ रहा है। • मुक्त चरागाही पद्धति (फ्री-ग्रेज़िंग) के कारण वनों में पौधों का पुनर्जनन प्रभावित हो रहा है। • बढ़ती पशु संख्या के कारण चारागाहों की कमी, जिससे पशु वन क्षेत्रों में घुसकर वनस्पतियों को नुकसान पहुँचाते हैं। • वनों के नष्ट होने से जैव विविधता प्रभावित होती है, और कई वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास समाप्त हो जाते हैं। • चारागाहों के लिए वन भूमि के अतिक्रमण से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए पशुपालन के आधुनिक तरीकों को अपनाना, नियंत्रित चरागाही प्रणाली लागू करना, और कृत्रिम चारागाहों का विकास आवश्यक है। |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 16, Issue 1, January-June 2025 |
| Published On | 2025-03-27 |
| Cite This | राजस्थान में वन संपदा का भौगोलिक विश्लेषण - PREM SHANKAR KIRAR - IJAIDR Volume 16, Issue 1, January-June 2025. |
Share this

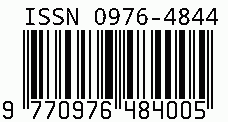
CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJAIDR DOI prefix is
10.71097/IJAIDR
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

